09-2-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:09-02-22
Facebook To Metaworse
Metaverse may not be Zuckerberg’s salvation if privacy violation is built into its business model
Apar Gupta, [ The writer is Executive Director, Internet Freedom Foundation ]
Over the past week Meta Platforms, which owns and operates Facebook, Instagram and WhatsApp, has taken a big market hit. Its shares $240 billion off its market capitalisation. As of Monday, this trend continued with another dip of 4. 7%, a cumulative stock price fall of 30% since its earnings report for the fourth quarter of 2021.
Is Meta’s share fall a part of the overall bearish market sentiment on because the Alphabet-Google stock is down only 1. 8% and the Amazon stock, after a drop, is now witnessing a rally. Therefore, markets are sending a bigger message to Meta.
Market analysts have set out two primary reasons for Meta’s challenges. The first is that Facebook has lost roughly half a million users, marking a decline in its global user base for the first time. While this may seem like a blip in the overall number of 1. 93 billion active daily users, if this continues as a trend, it will lead to a negative network effect.
The doctrine of network effects says that the value of a communications network is proportional to the square of the number of its connected users. Just as this plays out when most people join social media, a shrinking user base will usually have a compound impact that will spur greater attrition – simply, each person leaving Facebook, prompts another.
The justification provided by Meta in its earnings reports and investor calls have focussed on, “increased competition for people’s time”. This means that more social media users today prefer native video sharing platforms such as TikTok to Facebook, or even Instagram Reels.
The second reason is contained within the press release accompanying Meta’s financial results and states, “ We will overlap a period in which Apple’s iOS changes were not in effect and we anticipate modestly increasing ad targeting and measurement headwinds from platform and regulatory changes”.
This essentially means that Meta, an advertising company, is facing challenges targeting its users due to privacy protections and regulations on data protection. The most prominent has been due to technical changes in iPhones after iOS 14. 5, which lets users disable ad-tracking.
The response to these “headwinds” has been a mix of an intermediate solution and long-term product strategy. Immediately, Meta is focussing on video, and group messaging features to counter challenges from TikTok and similar platforms. It’s also devising new ways of ad delivery that are contextual and operate within the boundaries of ad-tracking blockers as those devised by Apple.
The longer term response is building a Metaverse. This will be possibly a constellation of immersive virtual reality environments that will serve as the next generation of social media interactions. While market analysts are forecasting uncertain capital expenditures and user adoption as concerns, there is a greater reason to consider privacy and data protection challenges.
Any immersive virtual reality environment is likely to have greater adhesion to users leading to greater data collection. For instance, take a user’s eye as an example. It is one of our many organs that will be digitised and then rendered within the Metaverse.
As per a framework released by XRSI, a non-profit organisation working on rights around virtual reality environments, tracking in the Metaverse may include, “eye opening and closure; eye movements; eye health; pupil properties; iris characteristics; eyelid and skin properties”. This list is far from exhaustive but neatly captures the scale, granularity and extent of data collection possible through the Metaverse.
To allay such concerns a founder’s letter by Mark Zuckerberg emphasises that, “Privacy and safety need to be built into the Metaverse from day one. So do open standards and interoperability. ” However, this intent may not be implemented in engineering design or business practises if the core economic model of serving ads through data collection does not change. Similar human rights concerns and larger business impacts will manifest in time if the core business that powered Facebook is adopted by Meta.
Continuing a harmful, tired approach would also mean taking on most regulators and national governments that are devising or enforcing privacy regulations.
Also, social media-generated problems like abuse, disinformation and social polarisation will be likely more severe in a virtual reality environment like the Metaverse, which will have the ability to render more vivid experiences and alter our sense of reality.
This strategy comes at a time when user trust in Meta is low thanks to regular public scandals, including revelations by whistleblower Frances Haugen in several complaints to the US Securities Exchange Commission. In her subsequent testimony to the US Senate she has stated that, “I’m here today because I believe Facebook’s products harm children, stoke division and weaken our democracy. ”
To avoid repeating the same mistakes, and therefore avoid user disapproval, Meta needs to look at the first principles around which social media was built and Metaverse will be built. Unless the business model changes, the Metaverse may be Metaworse for both Meta’s users as well as shareholders.

Date:09-02-22
राजनीति स्वच्छ कैसे हो जब बाहुबली ही वोटरों की पसंद
संपादकीय
एडीआर की रिपोर्ट में एक अजीब तथ्य नजर आता है। वे उम्मीदवार ज्यादा जीतते हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। शायद यही कारण है कि अपराधियों/बाहुबलियों को टिकट देना दलों की मजबूरी हो गई है। नतीजतन लोकसभा में पिछले दस वर्षों में आपराधिक मुकदमे वाले ‘माननीयों’ का प्रतिशत बढ़कर 30 से 43 हो गया और संगीन अपराध वर्ग में आने वाले सांसद 14 से 29 प्रतिशत हो गए। इस काल में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के जीतने की उम्मीद भी बिना आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार के मुकाबले साढ़े तीन गुना ज्यादा रही। जाहिर है वोटरों को बाहुबलियों या अपराधियों से गुरेज नहीं है बल्कि उन्हें लगता है कि ऐसे लोग चुनना बेहतर होगा, जो ‘दबंगई’ वाला व्यक्तित्व रखते हों। आंकड़े यह भी बताते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और क्षेत्रीय स्तर पर अन्नाद्रमुक ही ऐसी पार्टियां हैं, जिसके गैर-आपराधिक मामलों वाले ज्यादा उम्मीदवार जीतते हैं, जबकि भाजपा सहित सभी अन्य दलों- यहां तक कि वाम दलों- के मतदाता भी आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को ज्यादा चुनते हैं। इनमें सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां दोनों क्षेत्रीय दलों- शिव सेना और एनसीपी- के आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार के जीतने की संभाव्यता क्रमशः सात गुना और चार गुना ज्यादा होती है। भाजपा के भी आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशी ज्यादा जीतते हैं। संभव है कि राजनीतिक विद्वेष पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा हो और जो कार्यकर्ता आक्रामक तरीके से सरकारों का विरोध करते हों, उन पर फर्जी मुकदमे ठोके जाते हों। लेकिन जिन पर हत्या या दुष्कर्म जैसे संगीन मुकदमे हैं, वे जनता की पसंद कैसे बनते हैं? शायद नाकारा सिस्टम से परेशान जनता अपने नेता को ‘रोबिनहुड’ की तरह देखना चाहती है, जिसके बारे में अतार्किक कहावत थी कि वह धनिकों को लूटता है पर गरीबों पर रहमदिल है।
Date:09-02-22
हिजाब के सवाल पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
मुस्लिम छात्राएं हिजाब (शिरोवस्त्र) पहनें या न पहनें, इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक में जंग छिड़ गई है। मामला उडुपी जिले के एक कॉलेज में गरमाया है। मंगलवार को कर्नाटक के ही एक अन्य कॉलेज में हिजाब पहनकर आई एक मुस्लिम छात्रा को घेरकर नारेबाजी भी की गई, जो गलत है। पर यह मुद्दा ऐसा है, जिस पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने कहा है कि 1983 में पारित एक शिक्षा कानून के तहत छात्र-छात्राओं की वेशभूषा क्या हो, यह सरकार या वह शिक्षण-संस्था तय करेगी। इस प्रावधान के विरुद्ध कुछ लोगों ने अदालत में याचिका भी दायर कर दी है। उनका कहना है कि ऐसा प्रावधान नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। कोई आदमी क्या खाए, क्या पहने, किस करवट सोए- इस सबकी उसे स्वंतत्रता है। यह तर्क मोटे तौर पर ठीक ही लगता है लेकिन इसकी बारीकियों में उतरेंगे तो इसके कई पहलुओं से सहमत होना मुश्किल है।
यदि हर नागरिक को खाने, पहनने और बोलने की असीम स्वतंत्रता हो तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन हिजाब पहनने की स्वतंत्रता किसी खतरनाक श्रेणी में नहीं आती है। हिजाब क्या है? हिजाब सिर और सीने पर ढके जाने वाले कपड़े को कहते हैं। कभी-कभी उससे चेहरा भी ढक लिया जाता है और सिर्फ आंखें खुली रहती हैं। वह लगभग वैसा ही होता है, जैसे आजकल सभी लोग- औरत और मर्द- मुखपट्टी या मास्क लगाए रखते हैं। औरतें हिजाब, बुर्का और नकाब धारण करें, यह परंपरा अरबों में इसलिए चली थी कि वे अंग-प्रदर्शन से बचें। लगभग ऐसी ही परंपरा भारत के सभी धर्मावलंबियों में भी रही है, जिसे पर्दा और घूंघट की प्रथा कहा जाता है।
लेकिन अब हिजाब जैसी परंपरा का पालन इस्लामी देशों में भी घटता जा रहा है। अब से 50-55 साल पहले जब मैं काबुल विश्वविद्यालय में अनुसंधान कर रहा था तब मैं देखता था कि अफगान छात्राएं शॉर्ट स्कर्ट पहनकर आती थीं। वैसे स्कर्ट मैंने रूस, यूरोप और अमेरिका में भी नहीं देखे। ऐसे में वेशभूषा पर सवालों का उठना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन घूंघट और हिजाब को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। घूंघट और हिजाब का प्रावधान किसी भी धर्मग्रंथ में नहीं है। कुरान शरीफ में कहा गया है कि अपने घर की महिलाओं से कहिए कि जब वे बाहर निकलें तो अपने अंगों को ढककर रखें ताकि लोग उन्हें तंग न करें। वे बाहरी लोगों के सामने अपनी नज़रें नीची रखें। कुरान में यह जो कहा गया, वह बिल्कुल उचित था, क्योंकि उस वक्त के अरब देशों में मर्द अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने में ज्यादा संकोच नहीं करते थे। वेशभूषा में परिवार की स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतने के लिए इसलिए भी कहा जाता था, क्योंकि उस जमाने में इसे स्वेच्छाचारिता से जोड़ दिया जाता था।
भारत में पर्दा-प्रथा कहां थी? यह भी कुछ सदियों पहले ही चली। खास तौर से विदेशी आक्रमणकारियों के काल से! कई संत कवियों और महर्षि दयानंद ने पर्दा-प्रथा का डटकर विरोध किया था। लेकिन आधुनिक काल में जब हम स्त्री-पुरुष समानता की बात करते हैं तो सिर्फ स्त्रियों पर इस तरह के अतिरंजित बंधन क्यों थोपना चाहते हैं? यहां इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि स्त्रियां अपने अंगों का प्रदर्शन न करें यही ठीक है, इसी तरह इस मत के विरोधी पूछ सकते हैं कि वे अपनी पहचान भी क्यों छिपाएं? बुर्का, घूंघट, पर्दा, हिजाब और नक़ाब तो उनके चेहरे को भी ढक लेते हैं।
यदि कोई कुछ नहीं पहनकर बाहर निकले तो वह आपत्तिजनक जरूर है (दिगंबर संतों के अलावा), लेकिन कोई किसी भी रंग, शैली, आकार, कीमत का कपड़ा पहने तो उसमें आपत्ति का कारण नहीं बनता। यदि मुसलमान स्त्रियां बुर्का पहनें, हिंदू स्त्रियां घूंघट काढ़ें और माथे पर सिंदूर लगाएं, हिंदू पुरुष चोटी रखें, जनेऊ पहनें तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत में धोती, पाजामा, लुंगी, पेंट, चादर, अंगोछा आदि अधोवस्त्रों के कई रूप प्रचलित हैं। लेकिन शिक्षा-संस्थाओं को जाति, पंथ या मजहब की डोंडी पीटने वाले ऐसे प्रकट-चिह्नों से मुक्त रखा जा सके तो अच्छा है। इसीलिए भारतीय गुरुकुलों में समस्त ब्रह्मचारियों की वेशभूषा एक जैसी ही होती थी। यूनान के दार्शनिक प्लेटो की ‘एकेडमी’ और अरस्तू की ‘लीसीएम’ में छात्रों की वेशभूषा भी एक जैसी होती थी। चाहे वे किसी राजपरिवार के ही क्यों ना हों। सांदीपनि आश्रम में क्या कृष्ण और सुदामा अलग-अलग वेशभूषा में रहते थे?
कोई आदमी क्या खाए, क्या पहने, किस करवट सोए- इस सबकी उसे स्वंतत्रता है। यह तर्क मोटे तौर पर ठीक ही लगता है लेकिन इसकी बारीकियों में उतरेंगे तो इसके कई पहलुओं से सहमत होना मुश्किल है। यदि हर नागरिक को खाने, पहनने और बोलने की असीम स्वतंत्रता हो तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। हिजाब पहनने की स्वतंत्रता किसी खतरनाक श्रेणी में नहीं आती है। लेकिन अब हिजाब जैसी परंपरा का पालन इस्लामी देशों में भी घटता जा रहा है।
लोग अपने घर और बाजार में जैसी वेशभूषा पहनना चाहें, पहनें। उन्हें इससे भला कौन रोक सकता है? लेकिन शिक्षा-संस्थाओं में सबकी वेशभूषा एक जैसी हो तो उसके कई लाभ हैं। बचपन से लोगों में समता और सादगी का भाव पनपेगा। अमीरी की उच्चता ग्रंथि और गरीबी की हीनता ग्रंथि का भाव बच्चों में आपस की दूरियां पैदा नहीं करेगा। लेकिन जब लड़कियां हिजाब पहनेंगी, तो फिर भगवा दुपट्टा और नीला गुलूबंद भी दिखाई पड़ेगा। यह अलगाववाद चाहे मजहबी हो, जातीय हो या आर्थिक हो, शिक्षा-संस्थाओं में तो नहीं होना चाहिए। यदि मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी तो क्या उनके इस्लामी होने में कुछ कमी आ जाएगी? मैं जब इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था तो ब्रह्मचारी के नाते खड़ाऊ पहना करता था। जब प्राचार्य सी. डब्ल्यू. डेविड ने उसकी खट-खट पर आपत्ति की तो मैं उसे उतारकर नंगे पांव ही कालेज में प्रवेश करने लगा था। तब क्या मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो गया था?
हम छात्रों की वेशभूषा एक जैसी कर लें, तब भी अलगाव की समस्या रहेगी। उसे घटाने के लिए यह भी किया जा सकता है कि सारे भारतीय अपने खान-पान और नामकरण में भी मोटी-मोटी एकरूपता लाने की कोशिश करें। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी धोती-कुर्त्ता पहनें, दाल-रोटी खाएं और अपने नाम संस्कृत या हिंदी में रखें। विविधता कायम रहे लेकिन मुसलमानों के नाम सिर्फ अरबी, ईसाइयों के नाम सिर्फ इंग्लिश और यहूदियों के नाम सिर्फ हिब्रू में क्यों रहें? वे अरबों, अंग्रेजों और इजराइलियों की नकल क्यों करें? वे अपने नाम अपनी मातृभाषाओं में क्यों नहीं रखें? ऐसा होगा तो देश में अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाहों की संख्या बढ़ेगी और एकता इस्पाती बनेगी। मैंने इंडोनेशियाई मुसलमानों के नाम संस्कृत में देखे हैं। उनके राष्ट्रपति का नाम सुकर्णो था व उनकी बेटी का नाम मेघावती है। कुछ ही महीनों पूर्व सुकर्णो की एक अन्य पुत्री सुकमावती ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है और इसे इंडोनेशिया के मानवाधिकार और राजनीतिक चिंतकों ने अपने देश में धार्मिक बहुलतावाद का ही एक प्रमाण बतलाया था। बहरहाल, हिजाब वाले मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और माननीय न्यायालय के निर्णय से ही तस्वीर साफ हो सकेगी।

Date:09-02-22
खाद्य तेल आयात में कमी जरूरी
संपादकीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। परंतु महज कुछ ही दिन के भीतर सरकार ने तिलहन और खाद्य तेल की स्टॉक होल्डिंग पर रोक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उस चेतावनी की भी अनदेखी करता है जो आर्थिक समीक्षा में दी गई थी और कहा गया था कि अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़े ऐसे कदम उत्पादकों को गलत संकेत देते हैं। यह कदम कई वजहों से गलत समय पर उठाया गया है। मिसाल के तौर पर गत अक्टूबर में जब भंडारण सीमा की घोषणा की गई थी तभी से अधिकांश खाद्य तेलों की कीमत या तो स्थिर है या उसमें गिरावट का रुख है। बहरहाल, छह राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार ने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया और उस स्टॉक को अधिसूचित किया जो कारोबारी रख सकते हैं। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर शेष राज्यों पर भी प्रतिबंध लागू करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले भी एक गलत कदम उठाते हुए आयात शुल्क समाप्त करने और खाद्य तेलों पर लगने वाले कृषि उपकर को 20 फीसदी से कम करके केवल पांच से 7.5 फीसदी करने की घोषणा की गई थी।
इस मोड़ पर व्यापार प्रतिबंधों की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि रबी सीजन में तिलहन का बंपर उत्पादन होने की आशा है। रबी सीजन में तिलहन की प्रमुख फसल सरसों का रकबा 23 फीसदी अधिक होने का अनुमान है और अनुकूल मौसम होने के कारण फसल भी बहुत अच्छी होने की आशा है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक सरसों का उत्पादन 1.1 करोड़ टन से अधिक होगा जो पिछले वर्ष के 85 लाख टन से काफी अधिक है। ऐसे में अगर भंडारण पर कोई रोक लगाई जाती है तो खरीदार बाजार से दूर हो जाएंगे। इसका फसल कटाई के बाद के मौसम में कीमतों पर बुरा असर होगा जो उत्पादकों के लिए अच्छा नहीं होगा।
अगर किसानों को कमजोर कीमत मिलती है तो किसान अगले खरीफ सत्र में भी तिलहन की खेती करने से हिचकिचाएंगे और विदेशों से खरीद पर निर्भरता बनी रहेगी। पशुओं के भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले जीन संवद्र्धित सोयामील के आयात का हालिया निर्णय भी स्थानीय उत्पादन को हतोत्साहित करने वाला है। हमारा देश पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बन चुका है। हम अपनी 2.5 करोड़ टन तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए सालाना करीब 1.4 से 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात करते हैं।
व्यापक खपत वाली खाद्य तेल जैसी वस्तु के मामले में आयात पर इतनी अधिक निर्भरता उचित नहीं है क्योंकि ज्यादातर पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है। आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। इतना ही नहीं, हमारे देश में अपनी जरूरत का तिलहन और खाद्य तेल उत्पादित करने की पर्याप्त क्षमता है। सन 1980 के दशक के मध्य में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी जिसने इस दिशा में राह दिखाई थी। इसके तहत बाजार में तब तक किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया जब तक कि कीमतें एक तय दायरे में रहें और उत्पादकों तथा ग्राहकों के बीच संतुलन कायम रखें। बहरहाल, सन 1990 के दशक में इस नीति को त्याग दिया गया और मिशन का अच्छा काम अधूरा रह गया। एक बार फिर ऐसी ही नीति की आवश्यकता है ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाकर तिलहन एवं खाद्य तेल क्षेत्र के सभी अंशधारकों को लाभान्वित किया जा सके। इसमें उत्पादक, प्रसंस्करण करने वाले और उपभोक्ता सभी शामिल हैं।

Date:09-02-22
प्रतिभा की जगह
संपादकीय
अब इस बात पर उचित ही गर्व करते देखा जाता है कि सदियों से समाज के हाशिए पर डाल दी गई महिलाएं भी अपनी प्रतिभा के बल पर पुरुषों के समकक्ष खड़ी देखी जाने लगी हैं। इस क्रम में दुनिया की अनेक महिलाओं के उदाहरण दिए जाते हैं। मगर हमारे देश में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष भी जताया जाता रहता है कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के शीर्ष पदों पर महिलाएं नहीं पहुंच पातीं। इसमें पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को भी दोषी ठहराया जाता है। मगर अब ऐसी शिकायतें भी धीरे-धीरे छंटनी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की कतार में महिला न्यायाधीशों के खड़े होने से काफी संतोष और खुशी व्यक्त की गई। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति के रूप में शांतिश्री पंडित के चयन को भी देखा जा सकता है। वे इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति होंगी। चूंकि देश का यह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उस पर सबकी नजर रहती है। कई बार दबी या मुखर जबान में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि क्या वहां कोई ऐसी एक भी महिला प्रोफेसर नहीं हुई, जिसे वहां का कुलपति बनाया जा सके। दूसरे विश्वविद्यालय से ही सही, शांतिश्री पंडित के इस पद पर चयन से निस्संदेह ऐसे सवाल करने वालों को कुछ संतोष मिला होगा।
विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थान होते हैं। इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय की साख स्वाभाविक रूप से उसके कुलपति से जुड़ जाती है। कुलपति का नजरिया ही परिसर के परिवेश में दिखाई देता है। वहां होने वाली नियुक्तियों, शिक्षा सत्र और पढ़ाई-लिखाई के वातावरण, व्यवस्था आदि में कुलपति का व्यक्तित्व ही देखा-परखा जाता है। क्योंकि आखिरकार विश्वविद्यालयों की संपत्ति वहां के अकादमिक लोग ही होते हैं। मगर पिछले कुछ सालों से जिस तरह विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्तियों आदि को लेकर गुणवत्ता से समझौता होते देखा जाने लगा है, उससे कुलपतियों की नियुक्ति पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति भी विवाद से परे नहीं मानी जा सकतीं। इस पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले ही वे अनेक बार विवादों में घिरी रही हैं। महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में वे राजनीति विज्ञान की आचार्य हैं। वहां रहते हुए उन्होंने गांधी और गोडसे प्रसंग में ट्विटर पर एक तरह से गांधी-विरोधी टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर उन्हें तीखे विरोधों का सामना करना पड़ा था। इसी तरह उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में विरोध कर रहीं, धरने पर बैठी मुसलिम महिलाओं को फिदायीन कह दिया था। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की अगुआई करने वाले नेताओं को परजीवी कह दिया था।
यह ठीक है कि संविधान में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर जब समाज का कोई जिम्मेदार माना जाने वाला व्यक्ति हल्की बातें करता है, तो उस पर विरोध का स्वर उभरना स्वाभाविक है। शांतिश्री पंडित के पहले दिए गए उनके बयानों से उनकी विचारधारा और चीजों को देखने की दृष्टि का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। इसलिए अंगुलियां सरकार पर भी उठनी लाजिमी हैं कि उन्हें क्यों इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। खैर, मनुष्य के स्वभाव और सोच को लेकर उम्मीद की खिड़की कभी बंद नहीं होती। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी जिम्मेदार पद पर पहुंच कर व्यक्ति के कामकाज का तरीका पहले के अपने ढंग से उलट हो जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई कुलपति विश्वविद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगी।
Date:09-02-22
संकट में छोटे उद्यम
सरोज कुमार
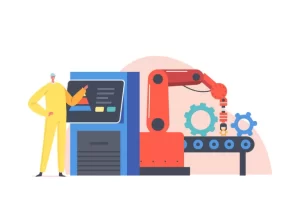 करोड़ों हाथों को काम देने वाले देश के छोटे उद्यम लंबे समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों ने उन्हें उजाड़ने का ही काम किया। महामारी ने छोटे उद्यमों को मृतप्राय कर दिया। सरकार की ओर से अभी तक किए गए बचाव के उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं। नए बजट से उम्मीदें थीं। लेकिन यहां भी उधार की उम्मीदें हैं। जबकि अभूतपूर्व बेरोजगारी के समय में छोटे उद्यमों को तत्काल आक्सीजन की जरूरत है।
करोड़ों हाथों को काम देने वाले देश के छोटे उद्यम लंबे समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों ने उन्हें उजाड़ने का ही काम किया। महामारी ने छोटे उद्यमों को मृतप्राय कर दिया। सरकार की ओर से अभी तक किए गए बचाव के उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं। नए बजट से उम्मीदें थीं। लेकिन यहां भी उधार की उम्मीदें हैं। जबकि अभूतपूर्व बेरोजगारी के समय में छोटे उद्यमों को तत्काल आक्सीजन की जरूरत है।
सरकार अब इस बात को मानने लगी है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझौले (एमएसएमई) उद्यम क्षेत्र पर महामारी का असर हुआ है। लेकिन असर का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। असर के आकलन के लिए पिछले साल नवंबर में निविदा आमंत्रित की गई थी। चयनित एजेंसी को दो महीने में एमएसएमई क्षेत्र की पिछले पांच साल की तस्वीर बतानी थी कि कितनी इकाइयां बीमार हैं, या बंद हुईं और कितनी नई खुली हैं। इस दिशा में कितनी प्रगति हुई, फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इस बीच लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के एक सर्वेक्षण में पता चला है कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड के दौरान सड़सठ फीसद एमएसएमई तीन महीनों तक अस्थायी रूप से बंद रहे, लगभग छियासठ फीसद इकाइयों का मुनाफा घट गया। 27 जनवरी, 2022 को आई इस सर्वे की रपट एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने तीन जनवरी, 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में साझा की। लेकिन सीमित दायरे के कारण यह रपट एमएसएमई क्षेत्र की पूरी तस्वीर पेश नहीं करती कि कितनी इकाइयां बीमार हैं या कितनी बंद हो गईं।
बीमार एमएसएमई इकाइयों की संख्या अंतिम बार 2017 में बताई गई थी। एमएसएमई राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने 11 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि पिछले चार वर्षों में बीमार एमएसएमई इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई। जवाब में आरबीआइ के आंकड़े के हवाले से कहा गया था कि वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बीमार एमएसएमई इकाइयों की संख्या दो लाख बाइस हजार दो सौ चार थी, जो 2015-16 के दौरान बढ़ कर चार लाख छियासी हजार दो सौ इक्यानवे हो गई। ध्यान रहे, यह आंकड़ा नोटबंदी से पहले का है। एमएसएमई इकाइयां ज्यादातर नकदी में कारोबार करती हैं, लिहाजा आठ नवंबर, 2016 को लागू हुई नोटबंदी से यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन प्रभाव का कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया। सरकार ने कोई आंकड़ा दिया नहीं, निजी एजेंसियों के आंकड़े को वह खारिज करती रही है। इसका एक अर्थ यह है कि एमएसएमई क्षेत्र की बीमारी को लेकर नीति-नियंता गंभीर नहीं थे। अब जब आंकड़े जुटाने की कवायद शुरू हुई है तो गंभीरता की बात समझ में आती है, और थोड़ी उम्मीद भी जगी है।
फिलहाल, एमएसएमई क्षेत्र की बीमारी का अंदाजा एनपीए के आकार से लगाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़े बताते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र का एनपीए वित्त वर्ष 2021 में बढ़ कर एक लाख अट्ठाइस हजार पांच सौ दो करोड़ रुपए हो गया, जो इसके पहले के वित्त वर्ष में एक लाख आठ हजार सात सौ चार करोड़ रुपए था। जबकि इसी अवधि के दौरान बैंकों का कुल एनपीए 7.1 फीसद नीचे आया और यह सात लाख अस्सी हजार पिच्चासी करोड़ रुपए हो गया है। बीमार इकाई उसे कहते हैं, जिसकी उधारी का खाता तीन महीने या इससे अधिक समय से एनपीए हो, या उसका नुकसान कुल पूंजी का पचास फीसद या उससे अधिक हो चुका हो।
सरकार ने बगैर किसी आंकड़े के ही बीमार एमएसएमई के इलाज के लिए महामारी के बीच मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) जैसे उपाय किए। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की छह जनवरी, 2022 को आई एक शोध रपट के अनुसार, ईसीएलजीएस के जरिए लगभग 13.5 लाख एमएसएमई खाते बचाए गए, जिनमें से 93.7 फीसद सूक्ष्म और लघु इकाइयों (एमएसई) के थे। परिणामस्वरूप एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए मूल्य का कर्ज एनपीए होने से बच गया। रपट में यह भी कहा गया है कि यदि ये खाते एनपीए हो जाते तो डेढ़ करोड़ श्रमिक बेरोजगार हो जाते। उल्लेखनीय है कि ईसीएलजीएस का लाभ पंजीकृत एमएसएमई ही ले पाते हैं, जबकि छह करोड़ तीस लाख एमएसएमई में से नब्बे फीसद से अधिक पंजीकृत नहीं हैं। अब इन गैर पंजीकृत इकाइयों में कितने बेरोजगार हुए होंगे, अंदाजा लगा लीजिए। आरबीआइ का ही दिसंबर 2021 का एक आंकड़ा कहता है कि सितंबर, अक्तूबर और नवंबर में एमएसएमई की बैंक ऋण वृद्धि दर नकारात्मक रही, जो क्रमश: -2.2 फीसद, -0.5 फीसद और -2.6 फीसद दर्ज की गई थी। यानी उद्यमों ने कर्ज लिया ही नहीं।
तमाम एमएसएमई इकाइयां अभी भी लाभ नहीं कमा पा रही हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को नए बजट से उम्मीद थी कि उन्हें कारोबार चलाने में मदद के लिए कोई सीधा लाभ दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर उन्हें उधारी की उम्मीद पकड़ा दी गई। ईसीएलजीएस की मियाद मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई और गारंटी कवर की सीमा साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से बढ़ा कर पांच लाख करोड़ रुपए कर दी गई। इसमें पचास हजार करोड़ रुपए आतिथ्य क्षेत्र और संबंधित उद्यमों के लिए है। सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट) योजना में आवश्यक धनराशि डाल कर उसे मजबूत करने की घोषणा की गई और कहा गया कि इस योजना के तहत एमएसई के लिए दो लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ वे एसएमई ले पाएंगे, जो ईसीएलजीएस के तहत ऋण के पात्र नहीं हैं। ईसीएलजीएस के तहत वही उद्यम कर्ज ले पाते हैं, जिनके ऊपर पहले का कोई कर्ज बकाया हो।
बजट में एमएसएमई की लागत घटाने के उपाय किए गए हैं। कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है या उसे घटाया गया है। वहीं, तैयार वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। जैसे इस्पात स्क्रैप पर पिछले साल सीमा शुल्क में दी गई छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि छातों पर सीमा शुल्क बढ़ा कर बीस फीसद कर दिया गया है और इसके कल-पुर्जे पर सीमा शुल्क छूट वापस ले ली गई है। लागत घटाने के ही उद्देश्य से एमएसएमई उत्पादों की सरकारी खरीद में लगने वाले बैंक गारंटी के विकल्प स्वरूप जमानती बांड स्वीकारने की सुविधा दी गई है।
बजट में सिर्फ आरएएमपी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी घोषित सभी पहलें पहले से ही चल रही हैं, जिन्हें विस्तार भर किया गया है। प्रश्न उठता है कि जब ये पहलें अभी तक एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ खास कर नहीं पाईं तो आगे की उम्मीद का आधार क्या है? आखिर दिक्कत कहां है? दरअसल, उठाए गए सभी कदम संगठित या पंजीकृत एमएसएमई पर केंद्रित हैं। ऐसी इकाइयों को इनसे लाभ भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। लेकिन पंजीकृत इकाइयां हैं कितनी? दस फीसद से भी कम। फिर नब्बे फीसद का क्या होगा? जबकि इन्हीं नब्बे फीसद को मदद की सबसे अधिक जरूरत है। एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, देश में लगभग छह करोड़ तीस लाख एमएसएमई में से मात्र सत्तावन लाख सड़सठ हजार सात सौ चौंतीस ही उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यदि गैर पंजीकृत उद्यमों की मदद नहीं की गई तो यह क्षेत्र कैसे बचेगा? फिर रोजगार कहां मिलेगा? देश की जीडीपी में लगभग उनतीस फीसद योगदान करने वाले, लगभग ग्यारह करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले एमएसएमई क्षेत्र की यह हालत देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपशकुन है।

Date:09-02-22
बेवजह का विवाद
अवधेश कुमार
पिछले कुछ समय में केंद्र और राज्यों के बीच एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले पर विवाद बना हुआ है जो सामान्य तौर पर नहीं होना चाहिए। यह विषय है, अखिल भारतीय सेवाएं यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा या आईपीएस और आईएफएस या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के केंद्र में प्रतिनियुक्ति। केंद्र सरकार ने हाल में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के नियमों में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए थे, जिसे लेकर कई राज्य आगबबूला हैं और इसे राज्यों के अधिकार का हनन मान रहे हैं। अनेक लोगों ने इस महत्त्वपूर्ण विषय को गहराई से समझें बिना टिप्पणियां करनी शुरू कर दी।
देश को यह पता होना चाहिए कि इस समय केंद्र सरकार अपने लिए अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। हाल में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आईएएस श्रेणी के इस समय कुल 223 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। सन 2011 में इनकी संख्या 309 थी। इस तरह एक दशक में 83 अधिकारियों की कमी हुई है। यह बहुत बड़ी संख्या है। बताया गया है कि आंकड़ा 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गया है। पुलिस सेवा में भी भारी संख्या में पद रिक्त हैं। वास्तव में केंद्रीय पुलिस संगठनों में अधिकारियों की कमी हो गई है। उदाहरण के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में डीआईजी स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा के 26 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 24 खाली है। कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होगी? सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस में भी डीआईजी के 38 में से 36 पद खाली पड़े हैं। चाहे सीबीआई हो आईबी सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों में यही स्थिति है। तो क्या यह संपूर्ण देश के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए?
वस्तुत: प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व होता है। उच्च पदों का यह 40 प्रतिशत है। इसी निर्धारित प्रतिशत से अधिकारी केंद्र में काम करने के लिए जाते हैं। परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार हर वर्ष ऐसे अधिकारियों की सूची मंगाता है जो केंद्र में आने की चाहत रखते हैं। बहुत सारे अधिकारी स्वयं भी केंद्र में जाना चाहते हैं और वो नियमानुसार राज्यों को अपनी इच्छा से अवगत कराते हैं, जो सूची केंद्र के पास पहुंचती है; उनमें से आवश्यकता अनुसार वे चयन करते हैं। पिछले कुछ वर्षो में राज्यों की ओर से इस सूची में काफी कमी की गई है और समस्या का यही कारण है। एक आंकड़ा उप सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों का है। इस समय उनकी संख्या 1130 है। 2014 में इनकी संख्या 621 थी, लेकिन प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों की संख्या केवल 114 है, जबकि 2014 में 117 था। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के बारे में बताया गया है कि कुल स्वीकृत पद 4984 है। इस समय 4074 अधिकारी उपलब्ध हैं। इनमें से केवल 442 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं जबकि नियमानुसार इनकी संख्या 1075 होनी चाहिए। इस तरह देखें तो आईपीएस में 633 अधिकारी कम है। राज्यों द्वारा की गई कटौतियों को देखें तो पश्चिम बंगाल ने 16 प्रतिशत, हरियाणा ने 16.13 प्रतिशत, तेलंगाना ने 20 प्रतिशत और कर्नाटक कर्नाटक 21.7 प्रतिशत अधिकारियों की कटौती कर दी है। अगर कटौती इतनी बड़ी संख्या में होगी तो इसका असर पड़ेगा। ऐसे में केंद्र के पास चारा क्या है?
केंद्र के पास रास्ता यही होता है कि वह राज्यों से सूची बार-बार मांगे। सूची न आने पर कुछ अधिकारियों का नाम अपनी ओर से भेजे ताकि राज्य उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए मुक्त कर सकें। राज्य इसके लिए तैयार नहीं हो तो फिर केंद्र के पास नियम बदलने के अलावा दूसरा चारा नहीं बचता। सच यह है कि केंद्र की ओर से राज्यों को बार-बार लिखा गया, लेकिन कई राज्य अधिकारियों को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में अनेक अधिकारी केंद्र में जाने के इच्छुक हैं, लेकिन राज्य सरकारें उन्हें मुक्त करने के लिए तैयार नहीं। इससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। 11 राज्यों ने केंद्र सरकार के ताजा प्रस्ताव (अधिकारियों को बुलाने का) का त्वरित विरोध करते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे पर प्रहार है। ध्यान रखने की बात है कि इस पत्र में यह भी कहा गया था कि कितने अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना है इस बारे में भारत सरकार राज्य सरकारों से सलाह करने के बाद ही निर्णय करेगी।
यह सोचने वाली बात है कि जब प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की सूची छोटी कर दी जाएगी तो केंद्र को नियम में बदलाव करना पड़ेगा और वह यही हो सकता है कि आप निश्चित समय सीमा में जो स्वीकृत पद हैं उसके लिए अधिकारियों को मुक्त करें। हां, इस पर सलाह-मशविरा हो सकता है। राज्य सहमत नहीं हो रहे हैं। 20 दिसम्बर 2021 के बाद 12 जनवरी और 17 जनवरी को केंद्र की ओर से दो अलग-अलग पत्र लिखे गए। 12 जनवरी का पत्र थोड़ा ज्यादा मुखर था। इसमें लिखा गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र अगर राज्यों से किसी विशेष अधिकारी की जरूरत बताता है तो राज्यों को उस अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। इसका विरोध ज्यादा हुआ है। यह विचित्र स्थिति है कि केंद्र सरकार को अपने ही देश में अपने लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों को लेने में समस्या हो रही है। यह ऐसा विषय है जो सामान्य तौर पर एक सहज स्वाभाविक चक्र के अनुसार जारी रहना चाहिए था। स्थापित नियम और परंपराएं हैं। देश केंद्र और राज्य दोनों के संतुलन से चलता है। यह संतुलन हर विषय में होना चाहिए। रास्ता यही है कि राज्य सरकारें नियमों के तहत अधिकारियों की जो संख्या निर्धारित है उन्हें केंद्र को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना चाहिए।
दुर्भाग्य से राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं, जबकि रास्ता यही है। बहुत सारे अधिकारी भी एक बार राज्य में स्थापित हो जाने या कुछ राजनीतिक नेतृत्व से संबंध बन जाने के कारण बाहर जाना नहीं चाहते। यह भी गलत है। उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा के लिए हुई है और सेवा देने के पीछे उनके अंदर यही भावना होनी चाहिए। वस्तुत: इस विषय पर टकराव और विवाद जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा। किसी अधिकारी को लेकर समस्या हो तो केंद्र राज्य बैठकर उसका रास्ता निकालें। यह प्रशासनिक आवश्यकता व दक्षता का मामला है जो सीधे-सीधे जनता के हितों से जुड़ा है।
Date:09-02-22
आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम
अभिषेक कृष्ण दुबे, ( लेखक भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं )
 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल दिशा-निर्देश और दूरगामी नीतियों का ही परिणाम है कि दो वर्ष कोविड महामारी से जूझने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आगे भी विकास की रफ्तार ऐसी ही बनी रहे, यह बजट सौ वर्ष की सबसे भयंकर आपदा के बीच विकास के नये विश्वास की लकीर खींचता है। मोदी सरकार का यह बजट न सिर्फ विकास की दूरगामी सोच को परिलक्षित करता है अपितु अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही आम जनता के लिए अनेक अवसर पैदा करने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल दिशा-निर्देश और दूरगामी नीतियों का ही परिणाम है कि दो वर्ष कोविड महामारी से जूझने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आगे भी विकास की रफ्तार ऐसी ही बनी रहे, यह बजट सौ वर्ष की सबसे भयंकर आपदा के बीच विकास के नये विश्वास की लकीर खींचता है। मोदी सरकार का यह बजट न सिर्फ विकास की दूरगामी सोच को परिलक्षित करता है अपितु अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही आम जनता के लिए अनेक अवसर पैदा करने वाला है।
सही मायनों में देखें तो बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकता व टेक्नोलॉजी की अनिवार्यता को पूरा करने का प्रयास वित्त मंत्री ने इस बजट में किया है। किसान ड्रोन, वंदेभारत ट्रेन, डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां या फिर 5जी सेवाओं की शुरुआत, अंतत: सबका लाभ देश के युवा, मध्यम वर्ग और समाज के निचले तबके में रहने वाले वंचित लोगों को मिलेगा। सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने गरीब कल्याण पर बजट में पूरा जोर दिया है। इस बजट ने गरीबों की आवास की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। केवल घर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक प्रत्येक गरीब को शुद्ध पेयजल की पूर्ति नल से हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी मूल आवश्यकताओं पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में मुख्यत: बड़ा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। गतिशक्ति मिशन के तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है। इस बार भी वित्त मंत्री ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, शिपिंग, बंदरगाह जैसे सात क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया है। इसीलिए वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति को सरकार की प्राथमिकता बताया है। इस संदर्भ में बजट के प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार अब इसमें निजी क्षेत्र की और भागीदारी बढ़ाना चाहती है। अर्थव्यवस्था की आधुनिक सोच के लिहाज से यह सही भी है कि सरकार को बिजनेस करने में नहीं उसे रेगुलेट करने तक सीमित रहना चाहिए। सरकार की इस सोच को वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में भी आगे बढ़ाया है। यही नहीं सरकार ने अपने बजट में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया है। बजटीय घोषणाओं में इस बात पर पूरा ध्यान दिया गया है कि हिमालय के समस्त क्षेत्र में जीवन आसान बने और वहां से लोगों का पलायन रु के। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में ‘पर्वतमाला योजना’ शुरू करने का ऐलान बजट में किया गया है। यह योजना पहाड़ों पर परिवहन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। यही नहीं बजट में मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस बार के बजट में कृषि को हाइटेक बनाने के साथ-साथ प्राकृतिक खेती पर भी फोकस है। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानी लाभप्रद हो, किसानों को नये अवसर मिलें। बजट में प्रस्तावित नये एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड और फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज जैसे प्रस्तावों से किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं किसान आंदोलन में मुद्दा बने एमएसपी के लिए वित्तमंत्री ने किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रु पये से भी ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर करने का प्रावधान किया है। साथ ही फर्टिलाइजर सब्सिडी को 79 हजार करोड़ से बढ़ाकर सीधा 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये किया गया है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र में अलग से सहकारी मंत्रालय बनने का ही नतीजा है कि इस बार बजट में सहकारी क्षेत्र को टैक्स में राहत मिल गई है। अभी तक सहकारी समितियों को 18 प्रतिशत वैकल्पिक कर जमा करना होता था, जबकि निजी कंपनियों के लिए इस कर की दर 15 प्रतिशत थी। इस बार के बजट में सरकार ने सहकारी क्षेत्र को निजी कंपनियों के बराबर ला दिया है। सहकारी समितियों को सरचार्ज के रूप में भी अब 12 प्रतिशत की बजाये केवल सात प्रतिशत सरचार्ज का भुगतान करना होगा। छोटे और मझोले उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कोरोना काल में छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने बीते दो वर्ष में कई निर्णय लिये हैं। कई तरह से इन उद्योगों को मदद पहुंचाई गई है। इस बजट में भी क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। रक्षा क्षेत्र में खरीद का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योगों के लिए आरक्षित करने का लाभ भी इन छोटे उद्योगों को मिलेगा। यह आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। यह बजट भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के साथ ही स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नये भारत की नींव डालेगा।

Date:09-02-22
देश विविधताओं से भरा, फिर कॉलेजों में विविधता क्यों नहीं
गौतम भाटिया, ( अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट )
बीती 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कॉलेज विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से वही पोशाक पहननी होगी, जिसे कॉलेज प्रशासनिक बोर्ड तय करेगा, और जहां ऐसी कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं हो पाती है, वहां वे कपडे़ नहीं पहने जा सकते, जिनसे ‘समानता, अखंडता और कानून-व्यवस्था के भंग होने’ का खतरा हो। यह आदेश विभिन्न कॉलेजों में घटी उन घटनाओं के संदर्भ में आया है, जिनमें हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इन घटनाओं के बाद कुछ लोगों का तर्क था कि हिजाब पहनना इस्लामी रवायत का एक जरूरी हिस्सा है, और इसकी मनाही संविधान से मिले ‘धार्मिक स्वतंत्रता’ संबंधी अधिकार का हनन है। तो, कॉलेज प्रशासन के फैसले के समर्थकों की दलील आई कि कॉलेज परिसरों को धर्म के किसी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन से मुक्त रखना चाहिए। इस तर्क को बल तब मिला, जब कई कॉलेजों में हिजाब की प्रतिक्रिया में कुछ हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनना शुरू कर दिया।
हालांकि, हिजाब और मजहब के दायरे में इस पूरे मसले को देखने वाले एक अहम बात को नजरंदाज कर रहे हैं, और वह बात है राज्य की ताकत; एक सार्वजनिक संस्कृति, और सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य पदानुक्रमिक समान विचार थोपने की राज्य व राज्य स्तरीय संस्थानों की ताकत। इसे अधिक ठोस रूप से कहें, तो यह सार्वजनिक जगहों पर वयस्कों (कुछ छात्र 18 से 20 साल के भी होते हैं) पर ‘ड्रेस कोड’ थोपने की राज्य संस्थानों की शक्ति का मसला है। हालांकि, मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं सार्वजनिक जगहों पर ‘सब कुछ’ की मंजूरी की कतई वकालत नहीं करने जा रहा। मसलन, राज्य के संस्थानों को यह अधिकार होना ही चाहिए कि वे ऐसे कपड़ों पर रोक लगाएं, जिन पर अशालीन या भड़काऊ नारे छपे हों, या जो शैक्षणिक संस्थान के लक्ष्यों से मेल नहीं खाते।
यहां सबसे अहम बात यह है कि हिजाब की एक सामाजिक प्रतीक के तौर पर कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है। कुछ मामलों में निश्चय ही यह धार्मिक दबदबे की अभिव्यक्ति है, और खुद चुनने से अधिक जबर्दस्ती थोपा गया प्रतीत होता है। मगर यह कहना कि हरेक औरत जबर्दस्ती हिजाब पहनती है या उनका ‘ब्रेनवाश’ किया गया है, पूरी मुस्लिम स्त्री-बिरादरी के वजूद को नकारना होगा। हिजाब पहनने के कई जटिल (और परस्पर विरोधी) कारण मौजूद हैं, जैसे- मुश्किल वक्त में अपनी पहचान छिपाने के लिए, परंपरा आदि। यकीनन, कुछ कारण मजहब से जुडे़ होंगे, लेकिन कुछ का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। लिहाजा, राज्य के लिए व्यक्तिगत स्तर पर यह सुनिश्चित करना कि वास्तव में असंभव है कि कोई किस वजह से हिजाब पहनता है?
यह तर्क हमें मूल मुद्दे पर वापस लाता है। यानी, हिजाब भेदभाव, असमानता या हिंसा का पोषण नहीं करता, जिसके आधार पर राज्य और उसके संस्थान किसी पोशाक को प्रतिबंधित करते हैं। एक तर्क यह भी सुनने में आता है कि शैक्षणिक संस्थानों में एक सीमा तक समानता की दरकार है। हालांकि, इस तर्क में भी कोई दम नहीं है, क्योंकि क्या यह उचित नहीं है कि हमारे शिक्षण संस्थान भी भारत की विविधता, बहुलता और विभिन्नता को प्रतिबिंबित करें, बजाय इसके कि इनको एकरूप बनाकर भारत के नैसर्गिक गुण को खंडित किया जाए? हमें तो अपने दैनिक जीवन में भी उन लोगों के साथ की दरकार होती है, जो हमसे दिखने में भिन्न होते हैं, अलग कपडे़ पहनते हैं और अलग जायके का खाना खाते हैं। तो फिर शिक्षण संस्थानों में यह विविधता बंद क्यों होनी चाहिए?
इन्हीं कारणों से कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि परिधान जैसे नितांत निजी मामलों में राज्य लोगों पर अपनी कितनी ताकत का प्रयोग कर सकता है? हमारा संविधान ऐसे व्यक्तिगत मामलों में सभी को ‘स्वतंत्रता’ की गारंटी देता है, जब तक कि इस आजादी से सामाजिक स्तर पर कोई बड़ा नुकसान न हो या सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा न मिले। हिजाब के मामले में हमें ऐसा कोई नुकसान होता नहीं दिखता। इसीलिए, कानून की कसौटी पर ऐसे प्रतिबंध खरा नहीं उतरते।

