30-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
 Date:30-04-22
Date:30-04-22
A step that would trigger language phonocide
Imposing Hindi would be catastrophic; instead, India would be better off having a multi-linguistic accommodative policy
Faisal C.K. is Under Secretary (Law) to the Government of Kerala.
The Union Home Minister, Amit Shah, recently urged the use of Hindi as the lingua franca, rather than English, in inter-State communication. He suggested (reportedly at the Parliamentary Official Language Committee) that when citizens of States who speak other languages communicate with each other, it should be in the “language of India”. It is quite natural that a leader of a political stream that raised the slogan, ‘Hindi, Hindu, Hindustan’ would air such a quixotic idea. It was V.D. Savarkar, the Hindutva icon, who first advocated the idea of Hindi to be declared the national language and articulated the slogan, ‘Hindi, Hindu, Hindustan’. R.V. Dhulekar, a member of the Constituent Assembly, bluntly stated in the Assembly, “You may belong – to another nation but I belong to Indian nation, the Hindi Nation, the Hindu Nation, the Hindustani Nation.”
India has a harmonious symphony of linguistic pluralism; it is not a disarranged cacophony. Ganesh N. Devy, in ‘Indigenous languages’, a UNESCO lecture in October 2008, and also in a media article, “Tribal languages in a death trap” in August 2011, has mentioned how Sir George Grierson’s Linguistic Survey of India (1903-1923) had identified 179 languages and 544 dialects in India. The 1961 Census reports mentioned a total of 1,652 ‘mother tongues’, out of which 184 ‘mother tongues’ had more than 10,000 speakers, and of which 400 ‘mother tongues’ had not been mentioned in Grierson’s survey, while 527 were listed as ‘unclassified’. In 1971, the linguistic data offered in the Census was distributed in two categories — the officially listed languages of the Eighth Schedule of the Constitution, and the other languages with a minimum of 10,000 speakers each. All other languages spoken by less than 10,000 speakers were lumped together in a single entry ‘Others’. That practice continued to be followed in subsequent enumerations. This practice made many languages invisible, says Prof. Devy.
Exposing a myth
The so-called ‘National Grandiosity’ of Hindi is a dubious fallacy unsupported by facts. Prof. Devy had exposed the myth of Hindi as a pan-Indian language. In an article in The Hindu on June 7, 2019, “Language, the opening move”, he wrote: “The 2011 Census data on languages, published last year, was heavily doctored. It presents Hindi as the ‘mother tongue’ of over 52 crore people by subsuming more than 5 crore claimants of Bhojpuri and more than 9 crore speakers of nearly 61 other languages — claimed as ‘other’ by their speech communities — from Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. ‘The Hindi’ is probably spoken by not more than 30% of the population, but it is not the mother tongue for the remaining 70%.”
Hindi is not a lingua franca for Indians; nor is it a dominant language. It is only a primus inter pares among numerous Indian languages.
In the neighbourhood
The imposition of one language in neglect of the others in a multilingual state is disastrous. Pakistan and Sri Lanka are textbook examples of how stubbornness over language ruined nations. After Partition and Pakistan was formed, Pakistan became a multi-ethnic and multi-linguistic state. In 1948, the Government of Pakistan ordained the Islamisation of East Pakistan, with Urdu as the sole national language. “There can only be one state language if the component parts of this state are to march forward in unison, and in my opinion, that can only be Urdu,” asserted Jinnah. This arrogance of the West Pakistan elite ignited the violent Bengali language movement or Bhasha Andolan in East Pakistan, advocating the recognition of the Bengali language as an official language of the then Dominion of Pakistan in order to allow its use in government transactions, in education, in media, in currency and to maintain its writing in the Bengali script. The Language Movement catalysed Bengali nationalism and the eventual separation of East Pakistan from Pakistan.
The Sinhala Only Act (the Official Language Act) of 1956 was a high point in Sri Lanka’s history. It triggered intense enmity and distrust between the Sinhalis and the Tamils. The Act replaced English with Sinhala as the sole official language of the nation with the exclusion of Tamil. Sinhalese was the language of Sinhalese people who formed 70% of the population. Tamil was spoken by Indian and Sri Lankan Tamils (and most Muslims) who together constituted around 29% of the country’s population. The Act was discriminatory and alienated the Tamil community from the mainstream. The Act also symbolised the Sinhalese majority’s zeal to assert Sri Lanka’s identity as a Sinhala nation state; for Tamils, it epitomised minority oppression and a justification for the demand for a separate Tamil nation. This friction sparked the decades-long civil war and ruined the nation.
A place for diversity
In contrast, the nations that accommodated linguistic diversity prospered. Singapore has a multi-ethnic population (Chinese, Malay and Indian). In its formative years, there was immense pressure to declare Chinese as the official language of Singapore. But Lee Kuan Yew, the architect of modern Singapore, quelled the demand and opted for English. English language proficiency made the city state a global business hub. In an article in The Straits Times (2004) he had said, “When we became independent in 1965, the Chinese Chamber of Commerce committee came to see me in my office, then at City Hall. They urged me to have Chinese as our national and official language. I looked them in the eye and said, ‘You must be mad, and I don’t want to hear any more of that from you. If you do, you are entering the political arena. I have to fight you. Because, Singapore will come apart.’ Supposing I had been otherwise inclined, which my colleagues would not have allowed, and had said, ‘Yes, okay.’ What would have happened to Singapore? Where would the Malays be, and the Indians, what future would they have? The English-educated Chinese would also be against us. The country would fall apart. Let us assume that we were all Chinese, no Malays, no Indians. Could we make a living with Chinese as our language of government and our national language? Who is going to trade with us? What do we do? How do we get access to knowledge? There was no choice.”
In South Africa, the national anthem of this Rainbow Nation, since 1997, is a five-language lyrical composition, making it the most unique anthem in the world in this regard. The languages are Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans and English. South Africa is an emerging leader of the African continent and its accommodative linguistic policy helped them a lot.
India should emulate the multi-linguistic accommodative policy of Singapore and South Africa; not the disastrous linguistic chauvinism of Pakistan or Sri Lanka. Imposing Hindi, which is the first language of the residents of only 12 of the 35 States and Union Territories (in the 2011 Language Census of India, and where Andhra Pradesh and Telangana figure together in the 2011 data) as a lingua franca would initiate the phonocide of other Indian languages. And it would prove to be catastrophic.
 Date:30-04-22
Date:30-04-22
क्यों बदलता जा रहा है देश का सामाजिक ताना-बाना?
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )
जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या आज भारत में सामाजिक खाई बढ़ती जा रही है, तो मैं तुरंत उन त्रासदियों के बारे में नहीं सोच पाता, जो इस तरह के प्रश्न को जन्म देती हैं- साम्प्रदायिक दंगे, मॉब लिन्चिंग, हिजाब, हलाल, अजान के लाउडस्पीकरों पर विवाद आदि- जिनका मकसद मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलना है। इसके बजाय मैं उन दो वाकियों के बारे में सोचने लगता हूं, जिनकी तरफ हाल ही में मेरा ध्यान खिंचा। इन्होंने उस बढ़ती हुई खाई को मेरे सामने कहीं अधिक स्पष्टता से चित्रित किया है।
पहला एपिसोड : हाल ही में जयपुर में मेरी मुलाकात लेबनान की एक महिला से हुई, जो बीते पंद्रह वर्षों से हस्तशिल्प और ज्वेलरी की डील्स के लिए भारत आ रही थीं। उनके बालों का रंग भूरा था और उन्हें देखते ही मालूम होता था कि वे विदेशी हैं। अतीत में हमेशा उनका स्वागत किया जाता रहा था। जब वे नूर के रूप में अपना परिचय देती थीं तो उनसे कहा जाता था कि कितना प्यारा नाम है, हमारे यहां भी ऐसा ही नाम हुआ करता है, हमें नूर शब्द का मतलब भी पता है- रोशनी। लेकिन वे कहती हैं कि आज चीजें बदल गई हैं। आज जब वे अपना नाम बताती हैं तो उनसे पूछा जाता है- ओह, तो क्या आप मुस्लिम हैं? यह प्रश्न जिस लहजे में पूछा जाता है, वह पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। अब वे सोच रही हैं कि शायद वे पहले की तरह नियमित रूप से भारत नहीं आएंगी।
दूसरा एपिसोड : एक पूर्व भारतीय राजदूत- जिन्होंने पाकिस्तान मामलों और इस्लामिक आतंकवाद के विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी- ने मुझे अपने एक दोस्त के बारे में बताया। वे काबुल के एक प्रतिष्ठित सर्जन हैं। अपने देश में तालिबान के बढ़ते प्रभाव से वे चिंतित थे और मेरे पूर्व राजदूत मित्र की सलाह पर उन्होंने पत्नी और बच्चों को भारत भेजने का निर्णय लिया (याद रहे उन्होंने उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा)। उन्होंने गुड़गांव में एक फ्लैट किराए पर लिया और बच्चों का नामांकन एक अच्छे स्कूल में कराया। लेकिन एक साल बाद ही उन्हें महसूस हो गया कि अब यह पहले जैसा भारत नहीं रह गया है। उन्हें सबसे गहरा आघात तब पहुंचा, जब उनके अपार्टमेंट में रहने वाले उनके बच्चों के दोस्तों ने कहा कि हमारे पैरेंट्स ने हमें आपके बच्चों के साथ खेलने से मना किया है, क्योंकि आप मुसलमान हैं। यह वाकया सुनाए जाने पर मेरे पूर्व राजदूत मित्र शर्मिंदा हो गए। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि बेहतर होगा वे अपने बच्चों को दुबई या लंदन ले जाएं।
मैं जानता हूं कि महज दो वाकियों के आधार पर आप किसी परिघटना का विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन एक-दूसरे से पृथक हाल ही की ये घटनाएं इस सच को उजागर करती हैं कि समाज में साम्प्रदायिक विभेद बहुत बढ़ गया है। आज सार्वजनिक मंचों से ऐसी बातें कही जा रही हैं, जिन्हें अतीत में परदे के पीछे भी कहा जाना उचित नहीं समझा जाता था। हेट-स्पीच इतनी आम हो चुकी हैं कि अब उन पर कोई चकित नहीं होता। एक समय था जब देश की केंद्र और राज्य की सरकारें कौमी एकता के प्रदर्शन के लिए कोशिशें करती थीं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। हिंसा की घटनाएं होने पर उन्हें भड़काने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती। अधिकारीगण इन घटनाओं की निंदा तक नहीं करते हैं।
मैं एक ऐसे भारत में बड़ा हुआ था, जहां गंगा-जमुनी तहजीब का उत्सव मनाया जाता था। लेकिन आज राष्ट्रवाद का मतलब बहुसंख्यकवाद होकर रह गया है। वहीं राष्ट्रीय एकता से आशय यह लगाया जाने लगा है कि वर्चस्वशाली समुदाय के नैरेटिव को सभी स्वीकार कर लें। पहले ‘अमर अकबर एंथनी’ जैसी फिल्मों को मनोरंजन-कर से मुक्त किया जाता था, जिसमें यह दर्शाया जाता था कि अपने माता-पिता से बिछड़े तीन बच्चों को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई परिवारों के द्वारा पाल-पोसकर बड़ा किया गया है। पहले दुनिया में इस बात के लिए हमारी इज्जत की जाती थी कि भारत के मुसलमान गर्व से हिंदुस्तान को अपना मुल्क बताते हैं और हमारी सफलताओं में उनका भी योगदान है। हम भी विदेशियों को नाज से बताते थे कि भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन तालिबान और अलकायदा से सहानुभूति रखने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन आज खाई ना केवल गहरा गई है, उसने हमारे समाज को भी बदला है। हम आशा ही कर सकते हैं कि आने वाला दौर हमें एकता की ओर ले जाएगा, विखंडन की ओर नहीं।
 Date:30-04-22
Date:30-04-22
हिंदी को कोसने की बुरी आदत
क्षमा शर्मा, ( लेखिका साहित्यकार हैं )
एक बार फिर हिंदी के साथ-साथ हिंदी वालों की पिटाई चालू है। आखिर हिंदी या हिंदी वालों ने दक्षिण या फिर अन्य क्षेत्र की किस भाषा का कब अपमान किया और किसे अपने मुकाबले दोयम दर्जे का कहा, लेकिन जब देखो तब, कभी चुनाव के मौके पर, कभी किसी मामूली सी बात पर हिंदी को कोसने, दुरदुराने और भला-बुरा कहने का नफरत भरा सैलाब आ जाता है। जब ऐसा होता है तब जो हिंदी के चलते अपनी रोजी-रोटी कमा सके, लेखक बन सके, बुद्धिजीवी, कलाकार कहलाए, वे लंबा मौन धारण कर लेते हैं। कोई बताएगा कि कब किस हिंदी भाषी राज्य में भाषा को लेकर दंगे हुए, जबकि दक्षिण में जिस तरह जब चाहे तब हिंदी भाषियों को खदेड़ा जाता है, लेकिन उनके अनुसार हिंदी वाले पिछड़े हुए हैं। उनकी कोई संस्कृति नहीं है। वे हिंदी साम्राज्यवाद दक्षिण पर लादना चाहते हैं। वे हिंदी भाषी जो 55 करोड़ हैं, उनकी दुर्गति ऐसी है कि कोई भी उन्हें आंखें दिखाकर चलता बनता है। हिंदी वाले चारों तरफ से लांछित होते हैं और इस डर से कि कोई उन्हें पिछड़ा न कह दे, चुप लगा जाते हैं।
यह केशवचंद्र सेन या महात्मा गांधी का जमाना नहीं, जो अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी के महत्व को स्वीकार करते थे। यह तो वह जमाना है कि बंगाल में एक डाक्टर ने बांग्ला न जानने के कारण एक महिला से कहा कि वह बिहार में जाकर ही अपना इलाज कराए। क्या अब डाक्टर, इंजीनियर तभी कोई काम करेंगे, जब उनका क्लाइंट उनकी ही भाषा बोलेगा? एक बार मशहूर लेखिका आशापूर्णा ने कहा था कि जब उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में हुआ, तभी उन्हें असली पहचान मिली। यही कहानी अन्य भाषा के दूसरे लेखकों की भी है।
दरअसल डर हिंदी से नहीं, उसके संख्या बल से है। उसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और उसके बड़े बाजार से है। यह कितना दिलचस्प है कि हिंदी वाले की जेब में दक्षिण के लोगों का हाथ तो घुसा होना चाहिए, हिंदी क्षेत्र के बाजार का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन न हिंदी चाहिए, न हिंदी वाले। अक्सर यह कहा जाने लगता है कि यदि हिंदी की बात तक की तो देश टूट जाएगा। भई वाह, आपकी भाषाओं की बात होती रहे, तब किसी हिंदी वाले को यह खतरा नहीं महसूस होता कि देश टूटने वाला है, लेकिन जैसे ही हिंदी की बात होती है, तो देश टूटने की धमकियां सी दी जाने लगती हैं। लगता है इस देश की अखंडता को बचाने की सारी जिम्मेदारी बस हिंदी वालों और हिंदी क्षेत्र की है। यदि आपको अपनी भाषा पर गर्व है तो यह गर्व किसी हिंदी वाले को क्यों नहीं होना चाहिए?
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया फिर से हिंदी विरोध में आ डटे हैं। पिछली बार जब कर्नाटक की एक मेट्रो ट्रेन में कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी स्टेशनों के नाम लिखे जा रहे थे तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। वह कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस कभी उनकी बातों का विरोध नहीं करती। क्या इसी तरह से यह दल उत्तर भारत में अपनी खोई जगह फिर से बना सकता है? एक बार जब मैसूर में उत्तर भारतीय यात्रियों की सुविधा के लिए रास्तों के नाम हिंदी में लिखने की कोशिश की गई थी, तब भी उसका विरोध हुआ था। वास्तव मे हिंदी तो उस गरीब की जोरू है, जिसे किसी न किसी बहाने हर बार पिटना है।
आखिर अजय देवगन ने क्या गलत कहा कि जब हिंदी से इतनी नफरत है तो अपनी फिल्में हिंदी में डब क्यों करते हो? भाषा के नाम पर घृणा भी फैलाएंगे और चाहेंगे कि न केवल पूरे भारत में छा जाएं, बल्कि ग्लोबल भी हो जाएं। आप कौन होते हैं, हमें पीटने वाले। आप भूल जाते हैं कि बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करने आते हैं। यदि आपकी बातों पर हिंदी के लोग आपकी ही तरह नाराज होने लगें तो? जब अजय देवगन के पक्ष में खड़े होने वाले नहीं दिख रहे, तब जाने-माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक बातचीत के दौरान खुलकर हिंदी का पक्ष लिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर बालीवुड में तीन चीजें बदलनी हों, तो वे क्या बदलना चाहेंगे। इस पर नवाज ने कहा कि पहले तो मैं बालीवुड का नाम बदलकर ‘हिंदी फिल्म इंडस्ट्री’ रखूंगा। दूसरा यह कि जो स्क्रिप्ट रोमन में आती है, उसे याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं देवनागरी में स्क्रिप्ट की मांग करूंगा। तीसरी बात यह कि जब फिल्म हिंदी में बन रही हो तब निर्देशक और उनके सहयोगियों का अंग्रेजी में बात करने का क्या तुक? उनके अनुसार इसके चलते एक्टर को आधी चीजें समझ में आती हैं, आधी नहीं। इससे परफार्मेस पर असर पड़ता है। दक्षिण भारतीय फिल्मों की यह अच्छी बात है कि निर्देशक और पटकथा लेखक से लेकर मेकअप करने वाला तक अपनी भाषा में बात करता है। वहां जो माहौल बनता है, उससे कुछ न कुछ नया निकलता है। सचमुच नवाज की बातों में दम है। उन्होंने एक नए विमर्श को दिशा दी है।
हिंदी की दुर्दशा के लिए हम लोग भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है। ज्यादातर हिंदी फिल्मों के सितारे अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। इसी तरह जब कोई हिंदी भाषी किसी उच्च पद पर पहुंच जाता है तो उसे हिंदी बोलने में शर्म महसूस होने लगती है। वह बड़े गर्व से कहता है कि ‘यू नो माई हिंदी इज नाट दैट गुड।’ अंग्रेजी के चरण चाटना इसी को कहते हैं। हिंदी का अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा से कोई विरोध नहीं, लेकिन विरोध न होने का यह मतलब भी नहीं कि आप अपनी श्रेष्ठता के नाम पर हिंदी और हिंदी भाषियों को हर बार नीचा दिखाएं। बहुत सह लिया अपमान, अब क्यों सहें?
 Date:30-04-22
Date:30-04-22
आत्मनिर्भरता की परिभाषा
संपादकीय
दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो ‘पूरी तरह अपने बलबूते पर हो’ और आत्मनिर्भर भारत वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं है। नेहरू के दौर में जब आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा था तब उसके चरम दौर में भारत मशीनरी से लेकर पूंजी और तकनीक से लेकर हथियार और यहां तक कि कलम भी आयात कर रहा था। जब स्वदेशीकरण के प्रयास रुके तो आयात पर निर्भरता बढ़ी। आज भी रक्षा और अंतरिक्ष जगत की अधिकांश ‘आत्मनिर्भर’ परियोजनाओं में ढेर सारी आयातित सामग्री इस्तेमाल की जाती है। तेजस लड़ाकू विमान में जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा है जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट कहती है कि उसके उपग्रहों में 50-55 फीसदी आयातित सामग्री लगती है। देश के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आयातित यूरेनियम पर निर्भर हैं। तेल की बात करें तो हम अपनी जरूरत का 85 फीसदी आयात करते हैं।
यदि आत्मनिर्भरता को नीतिगत रूप से विवेक संपन्न ढंग से इस्तेमाल करना है तो पहले इसे सही ढंग से परिभाषित करना होगा जबकि हमारी सरकार के मंत्री अक्सर ऐसा नहीं करते। क्या इसका अर्थ यह है कि सामरिक आयात पर निर्भरता कम की जाए या रूस जैसे प्रतिबंधों का खतरा कम किया जाए? इसका उत्तर अलग-अलग हो सकता है। एक ओर हरित क्रांति ने देश को अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के दबाव से निजात दिलाई जो सन 1960 के दशक में अकाल से जूझ रहे भारत को गेहूं की आपूर्ति करते हुए ऐसा कर रहे थे। तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से लेकर सौर ऊर्जा पैनलों तक आत्मनिर्भरता से जुड़ी परियोजनाओं का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं से मजबूत संबंध और घरेलू उत्पादन इकाइयों के लिए खतरा क्योंकि वे आयात पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान जेएफ-17 लड़ाकू विमान चीन के साथ साझेदारी में बनाता है। क्या ऐसा करने से पाकिस्तान चीन पर कम या ज्यादा निर्भर हो जाता है? क्या रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को तब भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब इसका मतलब आपूर्ति में देरी हो?
एक पुरानी कहावत है कैसे एक कील की कमी से एक साम्राज्य गंवा दिया गया। कील को घोड़े की नाल में ठोका जा सकता था और राजा घोड़े पर बैठकर युद्ध में जा सकता था…। कील खोजना आसान है जबकि छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कमी ने भारी भरकम ऑटोमोटिव सेक्टर को परेशानी में डाल दिया है। कल को कोबाल्ट या लिथियम की कमी से बैटरी उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हम खुद को पूरी मूल्य शृंखला के उतार-चढ़ाव से नहीं बचा सकते। व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता आधुनिक अर्थव्यवस्था में आम है। एक दलील यह है कि अपने देश में आपूर्तिकर्ता तलाशकर चीन जैसे शत्रु देश पर निर्भरता घटाई जा सकती है। लेकिन अधिकांश उत्पादों में चीन इकलौता आपूर्तिकर्ता नहीं है, हां वह प्रतिस्पर्धी कीमत वाला अवश्य है। वाणिज्यिक व्यापार में भारत उन देशों के साथ अधिशेष की स्थिति में है जो तेल उत्पादन नहीं करते। परिभाषा को व्यापक करके वस्तु एवं सेवा व्यापार को शामिल करें तो देश का चालू खाता घाटा सुरक्षित दायरे में है, विशुद्ध पूंजी की आवक घाटे की भरपाई की जरूरत से अधिक है, भारत ऊर्जा की कमी वाला देश है और हम चीन पर निर्भर हैं। हमारी समस्या वृहद व्यापार की नहीं है।
उस लिहाज से देखें तो विनिर्माण को व्यवहार्य बनाने में जरूर दिक्कत है और घरेलू क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के पीछे यही तर्क है। यदि पांच वर्ष तक सालाना 50,000 करोड़ रुपये खर्च करके देश में विनिर्माण क्षमताएं तैयार की जा सकें तो यह बहुत छोटी कीमत होगी। खतरा यह है कि स्थानीय मूल्यवर्धन शायद इतना बड़ा न हो कि सब्सिडी को उचित ठहराया जा सके, निर्यात प्रतिस्थापन लॉबी सरकार से विस्तारित अवधि तक सब्सिडी हासिल कर लेगी और संरक्षणवादी शुल्क से व्यापार उदारीकरण की स्थिति उलट जाएगी: इनमें से कुछ खतरे दिखने भी लगे हैं। वृहद आर्थिक जोखिम यह है कि ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी और तेल एवं रसायन आदि का इस्तेमाल करने वाले महंगी आपूर्ति करने वालों पर निर्भर हो जाएंगे। यह आत्मनिर्भरता के विपरीत बात होगी। पिछली बार कुछ ऐसा ही हुआ था और यह दोबारा हो सकता है। पीएलआई की दूसरी आलोचना यह है कि ये पूंजी के इस्तेमाल वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है, उनमें से कुछ को निरंतर तकनीकी और उपकरण संबंधी उन्नयन की जरूरत होती है। क्या यह व्यावहारिक है? इस बीच अपेक्षाकृत श्रम आधारित क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर संगठित रोजगार पैदा कर सकते हैं, वे अब भी पिछड़े हुए हैं। भारत के सामने व्यापार घाटे और रोजगार की कमी के दो संकटों में दूसरा संकट ज्यादा गंभीर है। पीएलआई के जरिये आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश में व्यवहार्यता तथा इस सवाल को भुलाया नहीं जाना चाहिए।
Date:30-04-22
‘गति शक्ति’ में दम, क्या समस्याएं कर पाएगी कम
इंद्रजित गुप्ता, ( लेखक फाउंडिंग यूल के सह-संस्थापक हैं )
‘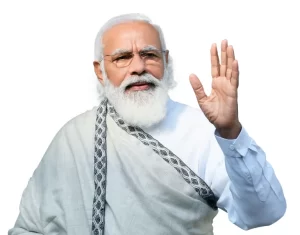 गति शक्ति’ योजना क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कुछ परियोजनाओं में एक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस योजना की शुरुआत की थी। भारत में बड़े आकार की ढांचागत परियोजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। परियोजनाओं में विलंब होने से समय एवं धन दोनों की हानि होती है। ‘गति शक्ति’ परियोजना का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इस पहल से ढांचागत क्षेत्र में कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
गति शक्ति’ योजना क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कुछ परियोजनाओं में एक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस योजना की शुरुआत की थी। भारत में बड़े आकार की ढांचागत परियोजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। परियोजनाओं में विलंब होने से समय एवं धन दोनों की हानि होती है। ‘गति शक्ति’ परियोजना का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इस पहल से ढांचागत क्षेत्र में कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
सरल शब्दों में कहें तो ‘गति शक्ति’ परियोजना भौगोलिक क्षेत्र का आकलन करने के लिए विभिन्न मंत्रालय एवं एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भू-अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल करती है। उपलब्ध तथ्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर यह नियोजन एवं क्रियान्वयन इकाइयों को एक ठोस सलाह एवं प्रस्ताव देती है। ‘गति शक्ति’ परियोजना विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ बाधाएं दूर करती हैं। हाल में प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया है कि इस परियोजना की शुरुआत के पहले छह महीनों में 131 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में ढांचागत कमियों का पता चला है और उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों का ध्यान आकृष्ट किया गया है।
हालांकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं लगता कि ‘गति शक्ति’ अभियान एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ऐसे लोगों का कहना है कि सूचना आधारित यह परियोजना ढांचागत विकास की राह में पेश आने वाली चुनौतियां दूर करने में कुछ हद तक ही योगदान दे सकती है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अधिकारी सूचनाओं के आदान-प्रदान में सक्रियता नहीं दिखाएंगे और पारदर्शिता लाने और नई पहल करने के प्रयास में बाधा पहुंचाएंगे। गति शक्ति पोर्टल में उद्योग जगत, खासकर परिवहन एवं ढांचागत खंड, के लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से गति शक्ति मिशन के तहत उपलब्ध कराई जा रही सूचनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। मगर यह स्पष्ट नहीं है कि निजी क्षेत्र गति शक्ति परियोजना से उत्साहित होकर ढांचागत परिायेजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित होगा या नहीं। वर्तमान में यह कहा नहीं जा सकता कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) प्रारूप के तहत सरकार की तरफ से किया गया भारी निवेश रंग लाएगा या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या गति शक्ति अपने वायदे पर खरा उतर पाएगी? या इसका भी हाल कुछ उन परियोजनाओं की तरह होगा जिनका उद्देश्य तो नेक था मगर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए?
इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें फिलहाल प्रतीक्षा करना होगी। हालांकि इस परियेाजना के संभावित लाभ तो दिख रहे हैं। नए मार्गों और इनमें आने वाले वन क्षेत्र और परिवहन के अन्य साधनों को एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत पर विचार करने में छह महीने की वजह कुछ ही ह ते लगेंगे। गति शक्ति परियोजना की मदद से वस्तुओं का परिवहन तेजी से हो सकता है जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में अधिक क्षमता सृजित होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। देश में मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से उत्तर प्रदेश में दादरी तक विशेष मालवहन गलियारा इसका एक विचारणीय उदाहरण है। उस समय सभी बड़ी रेल परियोजनाओं के लिए रेलवे के पास एक ‘ई-दृष्टि’ पोर्टल हुआ करता था। गति शक्ति परियोजना ई-दृष्टि का ही नया रूप है। मगर क्रियान्वयन की दिक्कत पहले की तरह ही बरकरार है। रेलवे अधिकृत सूचीबद्ध कंपनी कॉनकॉर इस मालवहन गलियारे के दोनों तरफ परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है। मगर क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र कांडला तक कोई उपयुक्त परिवहन संपर्क नहीं होने की वजह से इनमें ज्यादातर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इससे कॉनकॉर को अपने निवेश पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गति शक्ति पोर्टल समर्पित मालवहन गलियारा परियोजना को सबसे कम दूरी वाले मार्ग के बजाय कुछ वैकल्पिक मार्ग मुहैया करा सकता है जिससे पूर्वी हिस्से में वन या खनन क्षेत्र इसके आड़े नहीं आएगा। असल बात यह है कि नियोजन प्रक्रिया में कई मंत्रालय एवं एजेंसियां लगे होते हैं और इनमें प्रत्येक के काम करने का एक अपना तरीका होता है। उदाहरण के लिए कोई नया बंदरगाह तैयार करते वक्त रेल एवं सड़क संपर्क पर पर्याप्त विचार किए बन जाता है। गति शक्ति में इन खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस अभियान में विभिन्न मंत्रालयों को एक मंच पर लाकर खामियों की पहचान की जाती है और इसके बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिए कार्य को अंजाम देने एवं परिणाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तय किया जाता है।
कागज पर यह सभी चीजें तत्काल जरूरी लग सकती हैं मगर ये सरकार के मौजूदा कामकाज के तरीकों और सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करती हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परियोजना के साथ भी यही समस्या थी। जीएसटी व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद भी एक लंबे समय तक सरकार इस प्रणाली से मिलने आंकड़ों का बुद्धिमता से इस्तेमाल करने में अक्षम थी। इस समय कम से कम 18 मंत्रालय-इस्पात, रेलवे, बंदरगाह, अक्षय ऊर्जा आदि-हैं जो ढांचागत क्षेत्र से जुड़े हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि गति शक्ति अभियान से विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय बढ़ेगा और अति महत्त्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं को तो जरूर लाभ मिलेगा। पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव स्वयं अहम मंत्रालयों के अधिकार प्राप्त सचिव समूहों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भी पैनी नजर बनाए रखता है।
मगर देखने वाली बात यह होगी कि क्या मंत्रालय सभी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं, खासकर जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, से संबंधित सूचनाएं गति शक्ति मंच पर साझा करने के लिए पहल करते हैं या नहीं। वित्त मंत्रालय ने जोर दिया है कि सभी बड़ी परियोजनाएं गति शक्ति मंच से होकर गुजरेंगी और उसके बाद उन्हें धन मुहैया कराया जाएगा। समन्वय समिति द्वारा समस्याओं की पहचान किए जाने के बाद इस पर कदम उठाने का विशेष अधिकार वित्त मंत्रालय को होगा। गति शक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह एक उपयुक्त डिजिटल परियोजना निगरानी प्रणाली साबित होगी या एक और अधूरी सरकारी योजना बन कर रह जाएगी।
 Date:30-04-22
Date:30-04-22
सुरक्षा और चुनौतियां
संपादकीय
हाल के वर्षों में बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की सुरक्षा का मुद्दा एक महत्त्वपूर्ण और गंभीर चिंता के रूप में उभरा है। भारत के लिए यह ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि दशकों से दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। दोनों ही देशों के साथ भारत को युद्ध का सामना भी करना पड़ा है। यह भी कि पिछले तीन-चार दशकों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमापार से आतंकी गतिविधियां चला रहा है। दूसरी तरफ सीमा विवादों को लेकर चीन ने भारत के खिलाफ जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो पाना आसान नहीं है। गौरतलब है कि दो साल पहले गलवान घाटी में चीन ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें चौबीस भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद चीन ने वहां घुसपैठ कर ली और नया विवाद खड़ा कर दिया। देखा जाए तो इस तरह के विवाद अक्सर ऐसी नौबत पैदा करते रहे हैं जब युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात बन जाते हैं। ऐसे में कई बार दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सैन्य कार्रवाई भी अपरिहार्य हो जाती है। जाहिर है, इस तरह की सुरक्षा के लिए देश के पास चाक-चौबंद सैन्य तंत्र से लेकर अत्याधुनिक हथियार और कुशल रणनीति का होना भी जरूरी है।
हाल में भारत के वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी ने दिल्ली में एक सम्मेलन में त्वरित युद्धों के लिए तैयार रहने की जो जरूरत बताई है, वह देश की सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करती है। दरअसल भारत की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि बिना लंबे-चौड़े और अत्याधुनिक सैन्य तंत्र के देश की रक्षा कर पाना आसान नहीं है। भारत तीन तरफ समुद्रों से घिरा है और छह हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटीय सीमा है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ है। चीन लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। पूर्वोत्तर का संकट इसलिए भी ज्यादा बड़ा है कि यहां के राज्यों की सीमाएं म्यांमा से मिलती है। यह इलाका नशीले पदार्थों से लेकर हथियारों तक की तस्करी के रूप में जाना जाता है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद भी देश के लिए कम बड़ा संकट नहीं रहा है। पिछले कुछ सालों में एक खतरा यह भी बढ़ा है कि पाकिस्तान नेपाल और म्यांमा के रास्ते भी आतंकियों को भारत में घुसाता रहा है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की ऐसी हरकतें युद्ध के खतरों को बढ़ाने वाली ही प्रतीत होती हैं। इसलिए आपात हालात में युद्ध जैसी तैयारियां वक्त की जरूरत बन कर सामने आ सकती हैं।
हालांकि पूर्वी लद्दाख में और पाकिस्तान सीमा पर मिलने वाली चुनौतियों से भारत ने कई सबक लिए हैं। दोनों देशों से खतरे को देखते हुए भारत भी अपनी सुरक्षा मजबूत करने अब पीछे नहीं है। जहां तक बात है सेना को अत्याधुनिक हथियार और साजो-सामान मुहैया करवाने की, तो देश में ही हथियारों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कई उन्नत हथियारों, रक्षा प्रणालियों और उपकरणों के मामलों में अभी भी हम रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हैं। लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ रहे हैं। पनडुब्बी और पोत अब भारत में ही बन रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया, तो देश की सैन्य ताकत में भी इजाफा होगा और पड़ोसी राष्ट्र भी आसानी से आंख नहीं उठा पाएंगे।
Date:30-04-22
कैसे मजबूत बने पंचायती व्यवस्था
सुशील कुमार सिंह
सुशासन शांति और खुशहाली का परिचायक होता है। पंचायत एक ऐसी संस्था है जो सुशासन को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज व्यवस्था के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का संस्थानीकरण स्थानीय स्वशासन की दिशा में न केवल एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है, बल्कि लघु गणतंत्र की दिशा में भी व्यापक दृष्टिकोण है। इतना ही नहीं, यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की इच्छा का परिणाम भी है। गांव के विकास के बिना भारत की प्रगति संभव नहीं है, यह कथन कहीं अधिक पुराना है, मगर इसके नएपन से आज भी छुटकारा नहीं मिला है। जहां से शासन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती हो और समस्याओं को समझने तथा हल करने का जमीनी प्रयास संभव हो, वही पंचायत है।
पंचायत शब्द भारत के लिए नया नहीं है। यह प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। जब समावेशी ढांचा तैयार किया जाता है और उसके उद्देश्य तय किए जाते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था का खाका बनता है, तब पंचायत के मार्ग से ही गुजरना पड़ता है। पंचायत केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि गांव की वह जीवनधारा है जहां से सर्वोदय की भावना और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को समान होने का एहसास होता है। पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी नींव है, जिसकी शुरुआत दो अक्तूबर, 1952 को हुई थी। पंचायत जैसी संस्था की बनावट कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों का भी नतीजा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विफल होना, तत्पश्चात बलवंत राय मेहता समिति का गठन और 1957 में उसी की रिपोर्ट पर इसका मूर्त रूप लेना देखा जा सकता है। गौरतलब है कि जिस पंचायत को राजनीति से परे और नीति उन्मुख सजग प्रहरी की भूमिका में समस्याएं दूर करने का एक स्वरूप माना जाता है, आज वही कई समस्याओं में जकड़ी हुई है।
नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत के गठन की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से इसका अनुपालन सुनिश्चित करना न केवल इनका दायित्व था, बल्कि गांवों के देश भारत को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली भी बनाना था। इस मामले में पंचायतें कितनी सफल हैं, यह पड़ताल का विषय है। मगर लाख टके का सवाल यह है कि जिस पंचायत ने सबसे नीचे के लोकतंत्र को मजबूती दे रखी है, वही समस्याओं से मुक्त नहीं है। चाहे वित्तीय संकट हो या उचित नियोजन की कमी या फिर अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा पुरुष वर्चस्व के साथ जात-पांत और ऊंच-नीच ही क्यों न हो। हालांकि पिछले तीन दशकों में ये समस्याएं कम भी हुई हैं और पंचायती व्यवस्था ने यह सिद्ध भी किया है कि उसका कोई विकल्प नहीं है।
पंचायत और सुशासन का गहरा रिश्ता है। पंचायत जहां लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है और स्वायत्तता इसकी धरोहर है, वहीं सुशासन कहीं अधिक संवेदनशील लोक कल्याण और पारदर्शिता व खुलेपन से युक्त है। पंचायत की व्याख्या में क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूर्ण और विशिष्ट अधिकार निहित है। इसी अधिकार से उन दायित्वों की पूर्ति भी होती है जो ग्रामीण प्रशासन के तहत स्वशासन का बहाव भरता है। जबकि सुशासन एक ऐसी अवधारणा है जो बार-बार शासन को यह सचेत करती है कि समावेशी और सतत विकास के साथ बारंबार सुविधा प्रदायक की भूमिका में बने रहना है। 1997 का ‘सिटिजन चार्टर’ सुशासन की ही देन थी और 2005 का सूचना का अधिकार इसी का एक और अध्याय था। इतना ही नहीं, 2006 की ई-शासन योजना से भी पंचायतों को ताकत मिली है। सुशासन की अवधारणा 1992 में सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। हालांकि 1991 के उदारीकरण के बाद इसकी पहल भारत में भी देखी जा सकती है। सुशासन के इसी वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जा रहा था। संविधान के 73वें संशोधन में जब इसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तब दो अक्तूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से यात्रा कर रही यह पंचायत रूपी संस्था एक नए आभामंडल से युक्त हो गई। 1992 में हुए इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। गौरतलब है कि संविधान के इसी संशोधन में गांधी के ग्रामीण स्वशासन को पूरा किया गया। पंचायतों में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण इसी संशोधन के साथ सुनिश्चित कर दिया गया था, जो मौजूदा समय में पचास फीसद तक है।
देखा जाए तो तीन दशक पुरानी संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक बदलाव तो आया है। राजनीतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरुषों की सोच बदली है। बावजूद इसके विभिन्न आर्थिक-सामाजिक रुकावटों के कारण आंतरिक क्षमता और शक्ति को लेकर महिलाओं में भरोसा पूरी तरह बन गया हो, ऐसा कम ही दिखाई देता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यही सजावट है कि पंचायतें सामाजिक प्रतिष्ठा और महिला भागीदारी से सबसे ज्यादा भरी हुई हैं, मगर राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण, बाहुबल, जात-पांत और ऊंच-नीच आदि दुर्गुणों से पंचायतें भी मुक्त नहीं हैं।
समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन सुशासन की एक कड़ी है। इसलिए पंचायतों का उद्देश्य एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए, जहां सुशासन का प्रभाव हो, जिसमें पंचायत में पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा मिल सके, ताकि 11वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों को जनहित में सुनिश्चित कर ग्रामीण प्रशासन को सशक्त किया जा सके। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हर चौथा व्यक्ति अभी भी अशिक्षित है और पंचायत व सुशासन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ़ हैं। इससे उनको पंचायत के लेखापत्र नियम पढ़ने व लिखने में कई दिक्कत आती हैं। डिजिटल इंडिया का संदर्भ भी 2015 से देखा जा सकता है। आनलाइन क्रियाकलाप और डिजिटलीकरण ने भी पंचायत से जुड़े ऐसे प्रतिनिधियों के लिए चुनौती पैदा की है। हालांकि देश की लाखों पंचायतों को अभी डिजिटल तकनीक से जोड़ना बाकी है, साथ ही बिजली आदि की आपूर्ति का कमजोर होना भी इसमें एक बाधा है।
डिजिटल क्रांति ने सुशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। जहां एक तरफ डिजिटल लेन-देन में तेजी आई है, कागजों के आदान-प्रदान में बढ़ोत्तरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है, फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में दावों के निपटारे के लिए रिमोट सेंसिंग, कृत्रिम मेधा आदि का प्रयोग होने लगा है, वहीं ग्राम पंचायतों में खुले स्वास्थ सेवा केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, ताकि वे ग्राम स्तरीय उद्यमी बने। सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ही ई-गवर्नेंस कहलाता है, जिसका लक्ष्य आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए साक्षरता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों की ताकत है। बीते तीन दशकों में पंचायतें बदली हैं। इन सबमें एक प्रमुख बात यह रही है कि महिलाओं की स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ी है। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकारों की मौजूदगी किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। सुशासन की दृष्टि से भी देखें तो लोक सशक्तिकरण इसकी पूर्णता है और लोक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से देखें तो पंचायत में ये सभी खूबियां हैं। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मसलों और समस्याओं के निराकरण के लिए एक निर्वाचित सरकार हो, जिसे स्थानीय मुद्दों पर स्वायत्तता प्राप्त हो।
 Date:30-04-22
Date:30-04-22
हिंदी को कभी भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया
एस. श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )
 अभिनेता किच्चा सुदीप की एक छोटी-सी वीडियो क्लिप ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर आग लगा दी। इसकी वजह से भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर तीखी बहस शुरू हो गई है। एक तरफ, जहां यह शीतयुद्ध पुराने राग को अलापने जैसा रहा है, तो दूसरी तरफ, यह उन तथ्यों को सामने लाने में भी कामयाब रहा, जिसे आम लोग अमूमन बिसरा चुके हैं। यह पूरा विवाद किच्चा के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने शायद दक्षिण भारतीय फिल्मों, विशेषकर केजीएफ-2 की अभूतपूर्व सफलता से उत्साहित होकर यह कह दिया कि ‘हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही’। देखा जाए, तो तथ्य भी यही है कि हिंदी कभी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। यह अंग्रेजी की तरह केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है। मगर किच्चा ने चूंकि कोई लिखित ्क्रिरप्ट नहीं पढ़ी, इसलिए उनके शब्द अपने अर्थ से भटक गए। शायद वह कहना चाहते थे कि हिंदी फिल्म जगत के दिन लद गए हैं और अन्य भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों ने इसके दबदबे को खत्म कर दिया है।
अभिनेता किच्चा सुदीप की एक छोटी-सी वीडियो क्लिप ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर आग लगा दी। इसकी वजह से भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर तीखी बहस शुरू हो गई है। एक तरफ, जहां यह शीतयुद्ध पुराने राग को अलापने जैसा रहा है, तो दूसरी तरफ, यह उन तथ्यों को सामने लाने में भी कामयाब रहा, जिसे आम लोग अमूमन बिसरा चुके हैं। यह पूरा विवाद किच्चा के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने शायद दक्षिण भारतीय फिल्मों, विशेषकर केजीएफ-2 की अभूतपूर्व सफलता से उत्साहित होकर यह कह दिया कि ‘हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही’। देखा जाए, तो तथ्य भी यही है कि हिंदी कभी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। यह अंग्रेजी की तरह केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है। मगर किच्चा ने चूंकि कोई लिखित ्क्रिरप्ट नहीं पढ़ी, इसलिए उनके शब्द अपने अर्थ से भटक गए। शायद वह कहना चाहते थे कि हिंदी फिल्म जगत के दिन लद गए हैं और अन्य भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों ने इसके दबदबे को खत्म कर दिया है।
बहरहाल, मुंबई से अभिनेता-निर्माता अजय देवगन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी।’ मगर ऐसा कहते हुए वह यह भूल गए कि भारतीय संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है और हिंदी उन्हीं में से एक है। हालांकि, हिंदी को विशेषाधिकार हासिल है, क्योंकि यह केंद्र और कई राज्य सरकारों के कामकाज की आधिकारिक भाषा है। अन्य भारतीय भाषाएं भी आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन वे अपने-अपने राज्यों या क्षेत्रों तक सीमित हैं।
अजय देवगन को मातृभाषा, आधिकारिक भाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर करना चाहिए। जहां तक मातृभाषा की बात है, तो यह सबकी अलग-अलग होती है। हिंदी पट्टी में ही हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, लेकिन बृज, अवधी, भोजपुरी जैसी अलग-अलग भाषाएं भी इसी क्षेत्र में हैं। इसके अलावा, भारत में हजारों तरह की बोलियां भी हैं, जिनकी हम यहां चर्चा नहीं कर रहे। रही बात आधिकारिक भाषा की, तो भारत की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, और न यह कोई असामान्य बात है। कई देशों के पास आधिकारिक भाषा नहीं है। अमेरिका भी उन्हीं में एक है।
सोशल मीडिया पर जहां इन दोनों सितारों ने एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच लीं, तो राजनेताओं ने भी इसमें कदमताल मिलाना शुरू कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने जहां सभी को कश्मीर की याद दिलाई कि भारत विविधताओं का देश है, तो वहीं कर्नाटक के राजनेता, जिनकी नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, किच्चा के समर्थन में आगे आ गए और उनके बयान की सराहना करने लगे। कुछ समाचार चैनल तो गलत तर्कों के आधार पर हिंदी और अंग्रेजी के बीच तुलना करने लगे। एक एंकर का सुझाव था, ‘चूंकि 44 करोड़ भारतीय हिंदी बोलते हैं और महज 10 करोड़ अंग्रेजी में सहज हैं, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना देना चाहिए?’ वह दरअसल यह भूल रहे थे कि अंग्रेजी को हिंदी की तरह ही संपर्क भाषा माना गया है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं हिदी की तरह हैसियत की मांग करती रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो सभी भारतीय भाषाएं केंद्र सरकार की कामकाजी भाषा के रूप में अपनी मान्यता की इच्छुक हैं। अब चूंकि अनुवाद कार्य करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के आ जाने से कई भाषाओं में एक साथ संवाद करना संभव हो गया है, इसलिए यदि सरकार अपनी इच्छाशक्ति दिखाती है, तो सभी भाषाओं को समान दर्जा देकर भाषा का विवाद सुलझाया जा सकता है।
यह घटनाक्रम सोशल मीडिया की सीमाओं और उसके काले पक्ष को भी जाहिर करता है। इसके कई उपयोगकर्ता दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं। सच तो यह है कि भाषा एक भावनात्मक और संवेदनशील मसला है, जिसकी व्याख्या करने का काम सिने कलाकारों को छोड़ देना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि भाषायी और पहचान संबंधी विवाद ही पड़ोसी देश श्रीलंका में गृहयुद्ध के कारण बने थे। बेशक, बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ-1, केजीएफ-2 जैसी दक्षिण की फिल्मों में नयापन है, लेकिन हमें इनका आनंद लेना चाहिए, न कि इन फिल्मों की सफलता से हिंदी सीने जगत को चोट पहुंचानी चाहिए। हमारे देश के सिनेमा दर्शक ऐसी बेजा तुलनात्मक बहसों में नहीं उलझना चाहते।
Date:30-04-22
हमारे बाजार की सबसे सशक्त भाषा है हिंदी
उदय प्रकाश, ( प्रसिद्ध साहित्यकार )
भारत में हिंदी भाषा को लेकर विवाद नया नहीं है। जाने-माने अभिनेता अजय देवगन और कन्नड सिनेमा के बड़े स्टार किच्चा सुदीप के बीच भाषा को लेकर जो विवाद उठता दिखा, वह भी कदापि नहीं चौंकाता। इस विवाद पर बॉलीवुड का अपना नजरिया है, उधर, दक्षिण से कुछ और अलग आवाजें आ रही हैं। दूसरी भाषाओं के कलाकार व नेता भी विवाद में अपना योगदान दे रहे हैं।
हालांकि, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी को फैलाने और लोकप्रिय बनाने में बॉलीवुड की भूमिका रही है, लेकिन बॉलीवुड में हिंदी की स्थितियों व सीमाओं को भी समझना होगा। हिंदी ने जो स्नेह-दुलार फैलाया है, उसे समझना चाहिए, उसकी उदारता और मिलकर चलने की क्षमता को भी एक नजर जरूर देखना चाहिए।
राज कपूर की एक फिल्म है, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें शैलेंद्र का लिखा एक गीत है, ये पूरब है, पूरब वाले/ हर जान की कीमत जानते हैं/ मिल-जुल के रहो और प्यार करो/ एक चीज यही जो रहती है/ हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
आप पाएंगे कि उत्तर भारत या भारत विशेष रूप से गंगा केंद्रित रहा है और हम यही कहते आए हैं कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। वैसे तो इस देश में कृष्णा, कावेरी, सतलुज, झेलम, पेरियार भी हैं, और जन-जन में प्रिय राम तो सरयू किनारे ही पैदा हुए और उसी में समा गए, लेकिन एक भी गीत बॉलीवुड का आप बताइए, जो सरयू पर बना हो? बॉलीवुड में राम केसाथ भी गंगा नदी को ही याद किया जाता है। तो जो यह बॉलीवुड है, जहां भाषा को लेकर बहुत गंभीर दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।
मैं ट्विटर व अन्य जगह हिंदी पर छिड़ी ताजा बहस देख रहा था। हम राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजकाज की भाषा और मातृभाषा में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं, सबको एक साथ गड्डमड्ड कर दे रहे हैं। तमिलभाषियों पर आप हिंदी जितनी भी लादें, वे तो नहीं कहेंगे कि हिंदी मातृभाषा है। यह समझना होगा कि वास्तव में हमलोग बहुभाषी हैं। मिसाल के लिए, मेरी मां भोजपुर की हैं, पिता बघेली, गांव छत्तीसगढ़ी, तो मैं किस भाषा को कहूं कि ये मेरी मातृभाषा है? यहां हमें उदार होना चाहिए। हां, यह गर्व लायक सच है कि हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, दुनिया में तीसरे नंबर की भाषा है, कई देशों में बोली जाती है।
हम लोग खूब विविधता वाले गणराज्य हैं और काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरकर एक राष्ट्र या एक राष्ट्रभाषा बनती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तो अभी भी राज्यों का ही समूह है, वह आज भी उस तरह से राष्ट्र नहीं है, जैसी हमारे यहां धारणा बनाई जा रही है। वैसे भी, संविधान में कहीं नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। सभी राजभाषाएं हैं। अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी का भी विरोध होता रहा है। हम गौर करें, तो कहीं भी एक लोकप्रिय धारणा बनाई जाती है और लोग उसी को मानने लग जाते हैं। लोक मान्यता कुछ और होती है और वास्तविकता कुछ और। यह विरोधाभास कभी कम नहीं होगा। देश में एक समय था, जब रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर अंग्रेजी में लिखे नामों को रंग से पोत दिया जाता था और उनकी जगह हिंदी में लिखा जाता था। हिंदी के पक्ष में आंदोलन या राजनीति वगैरह भी कुछ हुई। हिंदी राजनीति की भाषा बन ही सकती है, लेकिन वैसी नहीं बन सकती, जैसी चीन में मंदारिन है या जापान में जापानी भाषा।
बहुत पहले देश में त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया था। पढ़ाई में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा रहे, लेकिन यह हुआ नहीं, हम अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के बीच उलझे रह गए। दुख होता है, जल्दबाजी में हिंदी के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, उन्हें संपर्क भाषा, राजभाषा, मातृभाषा का अंतर नहीं पता है। दक्षिण की ओर से उठने वाला हिंदी विरोध भी उचित नहीं है, लेकिन जब-जब आप हिंदी के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगे, तब-तब दक्षिण में विरोध होगा। हिंदी के पक्ष में सिर्फ ज्यादा आबादी से कुछ नहीं होता है।
अभी फिल्मों में देखिए, अजय देवगन की किसी भी फिल्म ने वैसी कमाई नहीं की है, जैसी दक्षिण की फिल्मों केजीएफ, आरआरआर इत्यादि ने की है। यह अच्छी बात है, दक्षिण की फिल्में हिंदी में भी आ रही हैं, तो हम स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए। आज हिंदी बाजार की सशक्त भाषा है, यह उत्तर से दक्षिण तक हर कोई जानता है। वास्तव में, हिंदी का विरोध कहीं नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, इसे कभी-कभी जान-बूझकर उभारा जाता है।

