(06-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:06-12-21
Cooperation awaits its ‘finding Raiffeisen’ moment
In India, government control has only increased, violating a core cooperative principle of political neutrality
G. Sreekumar, [ A former central banker]
‘Cooperation has failed, but cooperation must succeed,’ wrote the All India Rural Credit Survey Committee in 1954. These were the words of Venkatappiah, first Executive Director of Reserve Bank of India and member of the Committee. He later became Deputy Governor, and Chairman of State Bank of India, before chairing the Agricultural Credit Review Committee in 1969.
This verdict came five decades after the first cooperative legislation of 1904. The Governor of the Madras Presidency, Lord Wenlock, was the first to seriously attempt replicating European cooperatives in India. Madras was ideal for this experimentation as it had similar institutions in its Nidhis. Nicholson, appointed by Wenlock in 1892 to report on the possibility of their implementation, summed up his 1895 report in two words: ‘Find Raiffeisen’.
Pioneers in Europe
Nicholson was referring to Friedrich Raiffeisen, who along with compatriot Schulze-Delitzsch in Germany, and Luzzatti of Italy, pioneered cooperatives in Europe. Raiffeisen based them on the principles of self-help, self-governance, and self-responsibility. Known for their trustworthiness and resilience against financial crises, most were known as Raiffeisenbanks, spreading to other parts of Europe and America. Rabobank, the Dutch cooperative whose first two letters come from Raiffeisen, was the last triple A-rated bank.
Nicholson wrote that the ‘future of rural credit lies with those who being of the people, live among the people, and yet by their intelligence, prescience and energy, are above the people’. He used Raiffeisen ‘not as indicative of a particular person or system, but of the zeal, energy, patience and continuous devotion so thoroughly exemplified in that great reformer, and of the spirit of co-operation, thrift, self and mutual help so thoroughly developed in the above and similar systems…’
The story in India
Gilbert Slater, after joining Madras University in 1915 as its first Professor of Economics, went looking for the Raiffeisen that Nicholson’s province had. At the office of the Registrar of Cooperative Societies (RCS), he found the clerks sleeping, turbans placed next to inkpots, and no clue about the whereabouts of their boss, whose expertise was in the Tamil almanac.
Better days came with his successor, F.R. Hemingway, ICS, who brought in Dr. John Matthai as Officer on Special Duty. The first Indian with a doctorate in Economics from the London School of Economics, Matthai worked for a year in Ireland with Sir Horace Plunkett, an expert in cooperation. He later became Slater’s colleague, and India’s Finance Minister.
Sir Denzil Ibbetson, moving the Cooperative Societies Bill on October 23, 1903, had said that the Bill sought to create ‘small and simple credit societies for small and simple folk with simple needs and requiring small sums only’. He added that ‘co-operation must be built up from the bottom, and not from the top’. Plunkett, in his foreword to Eleanor Hough’s The Cooperative Movement in India (1932), commented that what India had was not a movement, but a policy. It was ‘created by ‘resolutions of the Central Government’ unlike Europe.
Matthai wrote in 1925 that the challenge was to loosen government grip on cooperation over the years. But, government control has only increased, violating a core cooperative principle of political neutrality. This reflects a collective failure of the political class.
After Independence, cooperative institutions became an instrument of planning and state action. Not surprisingly, the most successful Indian cooperatives such as the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (GCMMF)/Amul, where Matthai’s nephew, Verghese Kurien, became a Raiffeisen, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) and Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO), are outside government control. Globally, seven of the top 10 cooperatives by asset size are from the financial sector. The Indian financial sector is nowhere in the picture going by asset size. A few make it in the top 300 by turnover/GDP per capita, aided by a low denominator.
When a cooperative bank scales up, maintaining its cooperativeness is a challenge. Cooperatives have also become avenues for regulatory arbitrage, circumventing lending and anti-money laundering regulations. The committees which examined cooperative banking suffered from the top-down quality that Plunkett and others frowned upon. Recent initiatives such as an umbrella organisation for urban cooperatives and a new Ministry of Cooperation at the Centre threaten to further this approach in the absence of safeguards.
A check on RCS
First, the powers of the RCS need to be scaled back. A British Indian innovation, it failed to stick to its original role of a facilitator: a friend, philosopher, and guide to cooperative societies. In almost all States, the RCS has become an instrument of inspection and domination, one which imposes uniform by-laws, and amends them when individual societies do not fall in line.
Early pieces of legislation gave wide powers to the RCS as the laws were in an experimental stage. Moreover, the laws were simple and elastic so that they could cater to a region extending from present-day Pakistan to Myanmar. The RCS was empowered to grant exemptions considering local conditions. But, the position continued even after the Montagu-Chelmsford Reforms placed cooperation under the provinces in 1919. The RCS continued to hold sway after Independence. Some States even provide for across-the-board takeover of cooperative boards. There is a need to transfer work from the RCS to cooperative federations — as in Singapore.
Second, the rural-urban dichotomy in the regulatory treatment of cooperatives is specious and outdated. It perpetuates age-old divisions based on the nature of operations and population size. Such differences are immaterial when regulation is to be based on the cooperative nature of organisations.
Third, the regulation and the supervision of cooperative banks should move to a new body from the Reserve Bank of India (RBI) for urban banks and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for rural banks. The arguments for combining supervisory powers with the RBI do not hold good for cooperative institutions. Moreover, it will ensure a fresh look at the regulation of these institutions to which stringent regulations like that of the Basel Committee are not designed to apply. As for NABARD, the burden of inspecting rural cooperatives (and regional rural banks) is a distraction from its core mandate, apart from being a drain on resources.
The Netherlands experience
Fourth, lessons from the Netherlands, where cooperative banks owe their success to a segmented market, are pertinent. In India, adopting a multi-agency approach, especially after bank nationalisation, has affected the efficiency of both commercial and cooperative banks. Commercial bank-cooperative sector linkages at various levels could alternatively provide better synergies.
Venkatappaiah’s words still ring true. So do the words of Nicholson, nearly 13 decades after his report: “Find Raiffeisen.”
Date:06-12-21
न्यायपालिका बनाम विधायिका
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )
 भारतीय संवैधानिक व्यवस्था अद्वितीय है, जिसके विधायिका न्यायपालिका व कार्यपालिका जैसे तीन स्तंभ हैं। संविधान निर्माताओं ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया है। इस सिद्धांत को उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में भी स्पष्ट किया है। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी गरिमा है। वह संविधान का व्याख्याता और संरक्षक भी है। यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से भी शक्तिशाली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता परिसंघीय संबंधों से उत्पन्न मामलों तक सीमित है, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया है। जजों की नियुक्तियों के मसले पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नहीं गए। तब तक कोर्ट ने आयोग की विधिमान्यता को निरस्त नहीं किया था। संसद के दोनों सदनों व आधे से अधिक विधानमंडलों में उक्त आयोग से संबंधित 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। तब यह भारत की विधि का भाग था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बताकर निरस्त कर दिया था। संविधान में मूल ढांचे का उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने आधारिक लक्षण या अपरिगणित मूल अधिकार आदि कई नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किए। पता नहीं कि किन-किन क्षेत्रों में नए सिद्धांतों का विस्तार होगा। अंतिम निर्णय न्यायालय का है। संविधान संशोधन विधायिका का अधिकार है। विधायिका ने उसके सदुपयोग से नियुक्ति आयोग बनाया था। आखिरकार संवैधानिक विधि का निरसन विधायिका के क्षेत्रधिकार का अतिक्रमण क्यों नहीं है?
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था अद्वितीय है, जिसके विधायिका न्यायपालिका व कार्यपालिका जैसे तीन स्तंभ हैं। संविधान निर्माताओं ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया है। इस सिद्धांत को उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में भी स्पष्ट किया है। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी गरिमा है। वह संविधान का व्याख्याता और संरक्षक भी है। यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से भी शक्तिशाली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता परिसंघीय संबंधों से उत्पन्न मामलों तक सीमित है, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया है। जजों की नियुक्तियों के मसले पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नहीं गए। तब तक कोर्ट ने आयोग की विधिमान्यता को निरस्त नहीं किया था। संसद के दोनों सदनों व आधे से अधिक विधानमंडलों में उक्त आयोग से संबंधित 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। तब यह भारत की विधि का भाग था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बताकर निरस्त कर दिया था। संविधान में मूल ढांचे का उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने आधारिक लक्षण या अपरिगणित मूल अधिकार आदि कई नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किए। पता नहीं कि किन-किन क्षेत्रों में नए सिद्धांतों का विस्तार होगा। अंतिम निर्णय न्यायालय का है। संविधान संशोधन विधायिका का अधिकार है। विधायिका ने उसके सदुपयोग से नियुक्ति आयोग बनाया था। आखिरकार संवैधानिक विधि का निरसन विधायिका के क्षेत्रधिकार का अतिक्रमण क्यों नहीं है?
ताजा मसला विधायिका पर गंभीर टिप्पणी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि विधायिका कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती, जो कभी-कभी बड़े मुद्दों की ओर ले जाते हैं। इससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।’ संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र विधायिका की व्यवस्था दी है। कानून बनाना विधायिका का काम है। विधायिका के सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। वे सरकार बनाते हैं। विधायिका मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाती है। मंत्रिमंडल नीति निर्धारित करता है। विधायिका सदन में कार्यपालिका नीति की चर्चा करती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी संविधान में सुस्पष्ट है। मंत्रिपरिषद विधि बनाने या संशोधन के लिए विधेयक लाती है। विधेयक में संबंधित विधि का विस्तृत औचित्य बताया जाता है। सदन में चर्चा होती है। यह कहना गलत है कि विधायिका कानून के प्रभाव का अध्ययन नहीं करती।
भारतीय विधायी संस्थाओं ने अनगिनत उपयोगी कानून बनाए हैं। वे ‘कानून के प्रभावी आकलन’ के बाद ही अधिनियमित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ही कई निर्णय विधि बन जाते हैं। उनके प्रभाव दूरगामी होते हैं। बहुधा न्यायालयों के निर्णयों से बनी विधि अव्यावहारिक भी होती है। दलबदल विरोधी कानून में सुनवाई से लेकर निर्णय के अधिकार संसद व विधानमंडल के अध्यक्ष/सभापतियों पर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में ऐसी सुनवाई के लिए तीन माह का समय निर्धारित किया है। न्यायालयों में तमाम मुकदमें लंबी अवधि तक चलते हैं। न्यायपालिका ने अपने लिए मुकदमों के निस्तारण की कोई अवधि क्यों नहीं बनाई? बंगाल हिंसा और शाहीन बाग जैसे कई मसले हैं। न्यायालयों से अतिरिक्त सक्रियता की अपेक्षा थी। कई बार न्यायमूर्ति सरकार या वादी-प्रतिवादी को फटकारते हैं। उससे कार्यपालिका के वरिष्ठ अधिकारी भी आहत महसूस करते हैं।
संविधान दिवस पर आयोजित उसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने कहा, ‘यह न्यायाधीशों का दायित्व है कि वे अदालत कक्षों में अपनी बात कहने में अत्यधिक सावधानी/विवेक का प्रयोग करें। अविवेकी टिप्पणी भले ही भली मंशा से की गई हो, परंतु न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है।’ राष्ट्रपति की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने डेनिस बनाम अमेरिका मामले में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फ्रेंकफर्ट को उद्धृत किया है। फ्रेंकफर्ट ने कहा था, ‘अदालतें प्रतिनिधि निकाय नहीं हैं। ये लोकतांत्रिक समाज का अच्छा प्रतिबिंब बनने के लिए डिजाइन नहीं की गईं।’ न्यायपालिका की स्वतंत्रता अविनाशी है। इसका संरक्षण जरूरी है। राष्ट्रपति ने ठीक कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तब खतरे में पड़ जाती है जब अदालतें भावना संबंधी जुनून में झूल जाती हैं और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक दबाव के बीच चयन करने में प्राथमिक जिम्मेदारी लेना शुरू कर देती हैं।’
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि तमाम लोग मानते हैं कि अदालतें कानून बनाती हैं। यह गलतफहमी है, लेकिन सही बात यही है कि न्यायालयों के निर्णयों से बहुधा कानून निकलते हैं। ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ही एक नई प्रस्थापना आई कि ‘संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं। यदि संविधान संशोधन अधिनियम संविधान की आधारिक संरचना या ढांचे को प्रभावित करने वाला है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित करने का पात्र होगा।’ वस्तुत: संविधान के आधारिक लक्षण का कोई उल्लेख संविधान में नहीं। संविधान सभा में भी ऐसे विषय पर किसी चर्चा का संदर्भ नहीं। आधारिक लक्षणों की अंतहीन सूची एक कल्पना जैसी है। निष्पक्ष न्यायपालिका भी इसी सूची का अंश है और इसी आधार पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को न्यायपालिका ने निरस्त किया था। न्यायिक सक्रियता पर भी यदाकदा सवाल उठते हैं और निष्क्रियता पर भी। न्यायालय द्वारा एक मामले में सरकारी अधिवक्ता पर टिप्पणी की गई कि आप काम नहीं करेंगे तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन इसका अर्थ गंभीर है।
अगर विधायिका और कार्यपालिका अपेक्षानुसार काम नहीं करती तो क्या न्यायालय, कार्यपालिका व विधायिका का काम करेंगे? कभी ऐसा प्रतीत हो कि न्यायपालिका अपना काम नहीं करती तो क्या विधायिका न्यायपालिका का काम करने लगेगी? संविधान ने तीनों महत्वपूर्ण स्तंभों को कर्तव्य और अधिकार सौंपे हैं। सब अपनी सीमा में रहें, उसी में भारत का भविष्य उज्ज्वल है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था विचारणीय है। राष्ट्रपति जी ने उचित ही कहा कि न्यायपालिका में स्वतंत्रता-निष्पक्षता बनाए रखते हुए नियुक्तियों का श्रेष्ठ मार्ग खोजा जा सकता है। इस पर विमर्श होना चाहिए।

Date:06-12-21
भारत में हरित हाइड्रोजन की दिशा में बढ़े कदम
विनायक चटर्जी
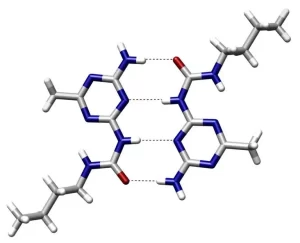 इस वर्ष जनवरी तक भारत में ऊर्जा पर परिचर्चा के दौरान हाइड्रोजन का खास जिक्र नहीं होता था। मगर फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन पर काफी चर्चा होने लगी है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ‘हाइड्रोजन मिशन’ के लिए 800 करोड़ रुपये के कोष का प्रावधान करने की घोषणा की थी।
इस वर्ष जनवरी तक भारत में ऊर्जा पर परिचर्चा के दौरान हाइड्रोजन का खास जिक्र नहीं होता था। मगर फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन पर काफी चर्चा होने लगी है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ‘हाइड्रोजन मिशन’ के लिए 800 करोड़ रुपये के कोष का प्रावधान करने की घोषणा की थी।
जून में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक में मुकेश अंबानी ने कहा था कि उनका समूह अपनी ऊर्जा नीति की दिशा में पहल करते हुए हाइड्रोजन पर बड़ा दांव खेलेगा और हरित (ग्रीन) हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए फ्यूल सेल और विद्युत अपघटन संयंत्र (इलेक्ट्रोलाइजर फैक्टरी) की स्थापना करेगा। इन दोनों घोषणाओं से बाजार हाइड्रोजन को लेकर अचानक उत्साहित हो गया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा, ‘अब भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन का है। मैं आज ‘राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन’ की स्थापना की घोषणा करता हूं। हमें हाइड्रोजन उत्पादन एवं इसके निर्यात के लिए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना होगा।’ सितंबर मध्य में अदाणी समूह ने दुनिया की सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करने की घोषणा कर डाली। इंडियन ऑयल ने मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की बात कही। एनटीपीसी ने भी लद्दाख में हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करने की योजना का खुलासा किया।
वायुमंडल में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है मगर वायु से हल्का होने के कारण एक गैस के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसे पहले जल जैसे दूसरे यौगिकों से अलग करना पड़ता है। यह प्रक्रिया पूरी करने के दो तरीके हैं जिनमें एक प्रक्रिया स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (एसएमआर) और दूसरी विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) है। विद्युत अपघटन में बिजली की अधिक खपत होती है। एक किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने के लिए करीब 50 यूनिट बिजली की जरूरत होती है। इसमें पूरे संयंत्र को चलाने और भंडारण एवं परिवहन पर आने वाली बिजली खपत इसमें शामिल नहीं है। अगर हाइड्रोजन पैदा करने के लिए बिजली का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के जरिये होता है तो इसमें फिर नई बात क्या है? जब जरूरी बिजली की मात्रा का उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से किया जाता है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें सह-उत्पाद जल होता है और इस तरह पूरी प्रक्रिया वातावरण के अनुकूल ईंधन की मदद से संपन्न होती है। लिहाजा हाइड्रोजन गैस के कई रूप होते हैं जो इसकी उत्पादन विधि पर निर्भर करते हैं। अगर इसका उत्पादन जीवाश्म ईंधन के जरिये होता है तो इसे ‘ग्रे हाइड्रोजन’ कहा जाता है जबकि जीवाश्म ईंधन के साथ मगर कार्बन कैप्चर तकनीक (वायुमंडल में कार्बनडाईऑक्साइड गैस प्रसारित होने से रोकने की प्रक्रिया) के साथ उत्पादन होता है तो इसे ‘ब्लू हाइड्रोजन’ कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर जब हाइड्रोजन उत्पादन होता है तो उसे ‘पिंक हाइड्रोजन’ कहते हैं।
इसी तरह, उत्पादन के आधार पर हाइड्रोजन को ब्राउन, ब्लैक, टरक्वाइज और पीला हाइड्रोजन आदि श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सभी दृष्टिकोण से उचित है मगर इस राह में उत्पादन लागत और परिवहन खर्च दो प्रमुख चुनौतियां हैं। जीवाश्म ईंधन से ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन पर 1 से 2 डॉलर खर्च आता है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत 4 से 6 डॉलर प्रति किलोग्राम है। ऐसा अनुमान है कि ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक ईंधन आधारित हाइड्रोजन के विकल्प के रूप में तैयार हो जाएगा। अंबानी ने सालाना आम बैठक में उम्मीद जताई थी कि एक दशक में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम होकर 1 डॉलर प्रति किलोग्राम रह जाएगी। परिवहन में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के विकल्प पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें भी काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिजली को हाइड्रोजन में तब्दील करने के बाद इसके परिवहन, भंडारण और फिर इसे बिजली में बदलने के बाद शेष बची ऊर्जा शुरुआती बिजली उत्पादन का 30 प्रतिशत से भी कम रह जाएगी। कुल मिलाकर यहां मुद्दा यह है कि हरित हाइड्रोजन के तेजी से उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की जरूरत होगी।
हाइड्रोजन का इस्तेमाल उद्योग, परिवहन और बिजली से जुड़े कार्यों मेंं होगा। परिवहन के झमेले से बचने के लिए कुल उत्पादन में करीब 85 प्रतिशत हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल तत्काल स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में धातु, अमोनिया और रिफाइनरियों में इस गैस का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन की लागत तेजी से कम करना एक सराहनीय राष्ट्रीय लक्ष्य है और सरकार को भी इसमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। सरकार उर्वरक, धातु और पेट्रोलियम परिष्करण में ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन लागू करना चाहती है और यह ठीक उसी तरह होगा जैसे रीन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) के मामले में हुआ था। शुरू में यह 10 प्रतिशत के स्तर पर शुरू हो सकता है और बाद के वर्षों में बढ़ाकर 20-25 प्रतिशत तक किया जा सकता है। भारी परिवहन में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मदद के रूप में अतिरिक्त रकम मुहैया करने पर विचार हो रहा है और संभवत: इसके उत्पादन के लिए उत्पादन संबद्ध योजना (पीएलआई) भी शुरू की जा सकती है। मसौदा बिजली नियम, 2021 में आरपीओ की आश्यकता पूरी करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की खरीदारी की अनुमति दी गई है। भारत हाइड्रोजन का महत्त्व और इसके अधिक से अधिक उपयोग की दिशा में समय रहते पहल कर चुका है। दुनिया में सालाना 12 करोड़ टन हाइड्रोजन उत्पादन होता है और इसमें केवल 1 प्रतिशत ही ग्रीन होता है। भारत में इस समय हाइड्रोजन की मांग करीब 60 लाख टन है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसमें 10 गुना बढ़ोतरी की जरूरत है। उद्योग, बिजली और परिवहन में यह क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और कार्बन युक्त ईंधन पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य में भी मददगार साबित होगा।


